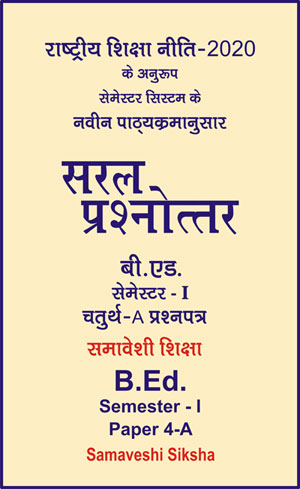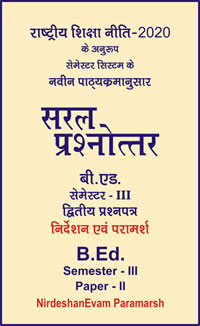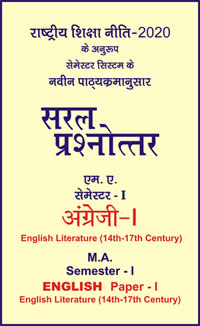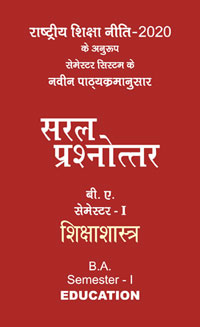|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- समावेशी शिक्षा में विभिन्न शिक्षण कौशलों का विवेचन कीजिए।
उत्तर-
अध्यापक का विकास व्यक्तिगत, अध्ययन विधियों, अध्ययन कौशलों पर निर्भर करता है कौशल कई विविध उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है। किसी भी विषय के विशेष उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अध्यापक के द्वारा विभिन्न कौशलों को अपनाया है। यह एक सूक्ष्म प्रक्रिया है जो शिक्षण और अधिगम को रोचक एवं प्रभावी बनाती है।
शिक्षण कौशल अध्यापक के उस व्यवहार समूह को कहते हैं जो छात्र-अध्यापक को नई बाह्य परिवर्तनों में विशेष रूप से प्रभावशाली सिद्ध होता है।
गेज के अनुसार - "कौशल नियोजित क्रियाओं की विशेष अनुशासन पद्धति व प्रक्रिया है, जिन्हें अध्यापक अनुभवजन्य प्रयोग करता है। शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं से या शिक्षण के कार्य के निरन्तर प्रवाह से सम्बद्ध होते हैं।"
मैकेन्टायर तथा वाइल्ड के अनुसार- "शिक्षण कौशल सम्बन्धित शिक्षण व्यवहारों का समूह है जो विभिन्न प्रकार की कक्षीय अन्तःक्रिया स्थितियों को उत्पन्न करता है जिससे विशिष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति में सुगमता होती है।"
समावेशी शिक्षा में शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक के द्वारा विषय-वस्तु की गहनता के अनुसार व विद्यार्थियों की रुचि, योग्यता व क्षमता के अनुसार विभिन्न कौशलों का प्रयोग करता है, जो निम्न हैं-
उद्दीपन परिवर्तन कौशल
उद्दीपन परिवर्तन कौशल इस सिद्धांत पर आधारित है कि उद्दीपन में परिवर्तन से ध्यान को आकृष्ट करता है एवं विद्यार्थी की अधिगम में रुचि उत्पन्न करता है। प्रायः यह देखा गया है कि उद्दीपन पर ज्यादा देर तक ध्यान स्थिर रखना कठिन होता है। अध्यापक को विशिष्ट बालकों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए शिक्षण कौशल में परिवर्तन होना आवश्यक है। विद्यार्थियों के ध्यान को आकृष्ट करने के लिए अध्यापक के व्यवहार को परिवर्तन कौशल कहा जाता है।
स्नेह जोशी के अनुसार- "विद्यार्थियों को उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करने और उसे बनाए रखने के लिए अध्यापक को कब, क्या और कैसे परिवर्तन करना है इसके लिए कौशल की आवश्यकता होती है। ऐसे कौशल को उद्दीपन परिवर्तन कौशल कहते हैं।"
पुनर्बलन कौशल
पुनर्बलन एक ऐसी तकनीक है जो अधिगम एवं व्यवहार प्रक्रिया को प्रभावित करती है। स्किनर के अनुसार- "यदि किसी अधिगम के प्रयास पर पुनर्बलन प्रदान किया जाए तो उसकी शक्ति बढ़ जाती है।"
पुनर्बलन दो प्रकार का होता है-
-
सकारात्मक पुनर्बलन - यह पुनर्बलन वांछनीय व्यवहार को सशक्त बनाकर कक्षा में विद्यार्थियों की सहभागिता में वृद्धि करता है।
-
नकारात्मक पुनर्बलन - यह पुनर्बलन विद्यार्थियों के अवांछित व्यवहारों को निरस्तारित कर उनमें अपेक्षित सुधार लाने में सहायता करता है।
सकारात्मक पुनर्बलन का प्रयोग जितना लाभदायक होता है, उसका गलत उपयोग उतना ही हानिकारक होता है।
पुनर्बलन कौशल से अध्यापक ऐसी शिक्षण तकनीक से है जिसके द्वारा एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों के व्यवहार में बाह्य परिवर्तन लाने हेतु पुनर्बलकों का उचित चुनाव और उनके प्रभावशाली उपयोग में पूरी-पूरी सहायता मिलती है।
व्याख्या कौशल
इस कौशल के द्वारा विषयवस्तु को सरल, स्पष्ट तथा सुलभ बनाया जाता है। इसका प्रयोग कक्षा में विभिन्न स्तर पर प्रश्न, दृष्टि-श्रव्य सामग्री तथा उदाहरणों की सहायता से विषयवस्तु को व्याख्या के लिए किया जाता है।
किसी व्यक्ति या किसी विचार, अवधारणा, नियम, अथवा क्रिया का बोध कराना व्याख्या कौशल कहलाता है। शिक्षण कौशल के और इसके मुख्य तत्वों में तथ्य हैं-
(i) विद्यार्थियों की आयु, पारिवारिक पृष्ठभूमि एवं ज्ञान के अनुसार तथ्य, अवधारणा, नियम आदि के अनुरूप उचित कथनों का चयन करना।
(ii) अवधारणा, विचार अथवा घटना को समझाने के लिए चुने हुए कथनों में अन्तरसंबंध स्थापित करना और उनका प्रयोग करना।
व्याख्या को प्रभावशाली बनाने के लिए अध्यापक को बाह्य व्यवहारों में वृद्धि कर अवांछित व्यवहारों से बचना होता है।
श्यामपट लेखन कौशल
श्यामपट अथवा चॉकबोर्ड महत्वपूर्ण दृश्य साधन है। इसका प्रयोग अध्यापक अपने पाठ को सरल, रोचक एवं आकर्षक बनाने के लिए करता है। अध्यापक को श्यामपट प्रयोग करने की कला में दक्ष होना चाहिए जिससे वह इसका प्रयोग करके शिक्षण को सफल बना सके।
उदाहरणों द्वारा दृष्टान्त कौशल
कुछ अवधारणाएँ इतनी अमूर्त होती हैं कि व्याख्या की सहायता से विशेष बालक उसे ठीक से नहीं समझ पाते। ऐसी परिस्थितियों में एक कुशल अध्यापक विचार, अवधारणा व सिद्धान्त की व्याख्या करने के लिए उदाहरणों का प्रयोग करता है।
उदाहरण सहित दृष्टान्त कौशल एक ऐसी कला है जिसके द्वारा अध्यापक अनुकूल उदाहरणों का न्याय संगत चयन करता है और विद्यार्थियों को समुचित ढंग उन्नत रूप से प्रस्तुत करता है ताकि वे सम्बन्धित विचार, अवधारणा, सिद्धान्त आदि को अच्छी तरह समझ सकें और उनका उचित प्रयोग कर सकें।
उदाहरणों द्वारा दृष्टान्त कौशल में मुख्यतः दो प्रक्रियाएँ निहित होती हैं-
- विद्यार्थियों के समक्ष किसी विचार अथवा सिद्धान्त को स्पष्ट करना।
- इस बात की पुष्टि करना कि विद्यार्थियों ने उस विचार को अच्छी प्रकार समझ लिया है या नहीं।
विवरण कौशल
विशिष्ट बालकों के कविता, कहानियों आदि का विवरण देकर शिक्षण शिक्षण को रोचक बनाता है।
विवरण का अर्थ है - कहानियों सुनाना या घटनाओं का वर्णन करना।
पैटन के अनुसार, विवरण अपने आप में एक कला है, जिसका लक्ष्य वाणी के माध्यम से विद्यार्थियों को समुचित स्पष्ट, रोचक एवं विधिवत क्रम से घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करना है कि वे अपनी कल्पनाओं में उनका पुनर्निर्माण कर सकें वे स्वयं उनके दर्शन करें या उनमें भाग ले रहे हों।
विवरण कौशल वह कला है जिसके द्वारा अध्यापक अन्तरसंबंधित कथनों की सहायता से कोई तथ्य, नियम, सिद्धान्त का बोधगम्य कराता है। यह एक शैक्षिक कौशल है जिसके दो प्रमुख तत्व हैं-
- विद्यार्थियों की आयु, परिवेशगत एवं पूर्व ज्ञान के अनुकूल तथा अवधारणा, नियम, घटना के अनुरूप उचित कथनों का चयन करना।
- अवधारणा, विचार अथवा घटना आदि के बोध के लिये चुने हुए कथनों में अन्तरसंबंध स्थापित करना व उनका प्रयोग करना।
विवरण कौशल में तीन प्रकार के कथन प्रयुक्त होते हैं-
- वर्णात्मक कथन
- विश्लेषणात्मक कथन
- तर्कात्मक कथन
कथात्मक कौशल
छोटी कक्षाओं में शिक्षण के लिए कथात्मक कौशल का प्रयोग बहुत उपयोगी एवं प्रभावशाली है। प्राथमिक कक्षाओं में बच्चों को प्राचीन समय के महान पुरुषों तथा स्त्रियों की प्रसिद्ध शासकों, सुधारकों साधुओं, वैज्ञानिकों तथा व्यापार की कहानियां सुनाई जा सकती हैं। बालक स्वभावतः कहानियां प्रिय होते हैं। अध्यापक के अंदर इस कौशल का होना अनिवार्य है। इस कौशल के प्रयोग के लिए अध्यापक की कल्पना शक्ति उत्तम हो, अतीत का उचित तथा पूर्ण ज्ञान हो और अलग-अलग के अनुभवों का प्रयोग के लिए उपयुक्त संग्रह हो। कक्षा-कक्ष में कौशल ऐसी कला है, जिसके द्वारा अध्यापक जीवंत कहानी का वर्णन करता है और उसे विद्यार्थियों के सामने उचित रूप से प्रस्तुत करता है ताकि समस्याओं, विचार, अवधारणाएं आदि को अच्छे तरह समझ सकें और उनके आदर्शों का अनुसरण करने की प्रेरणा प्राप्त कर सकें।
अभिनय कौशल
विशेषः बालकों के शिक्षण में अभिनयकला अथवा नाटकीयकरण का शिक्षण में बहुत अधिक महत्व है। सही और उचित समय पर किया गया अभिनय शिक्षण को अधिक रोचक, सरल एवं प्रभावपूर्ण बनाने में सहायता करता है।
नाटकीयकरण का अर्थ है - किसी तथ्य, कथानक या भाव को अंग संचालन या चेहरे पर दर्शाए गए हाव-भाव द्वारा समझाना। नाटकीयकरण एक कला है जो विद्यार्थियों की कल्पना शक्तियों को विकसित करने में सहायक होता है। इसके द्वारा बच्चों में सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। अभिनव कौशल के प्रयोग द्वारा शिक्षक अच्छा हो सकता है तो इससे केवल बालकों की अभिनव शक्तियों का विकास ही नहीं होता बल्कि बालकों का सम्पूर्ण व्यक्तित्व निखरता किया जा सकता है। स्वाभाविक विकास से सृजनात्मक शक्तियों का विकास भी होता है। अभिनय कौशल के द्वारा शिक्षक विषयवस्तु को रोचक, बनाकर आसानी से समझा सकता है।
|
|||||

 i
i