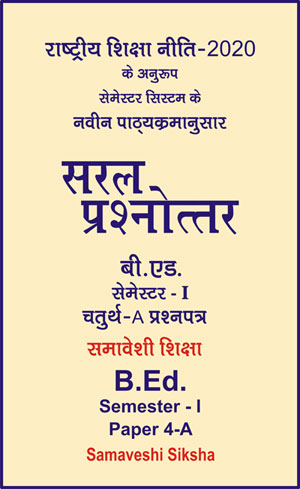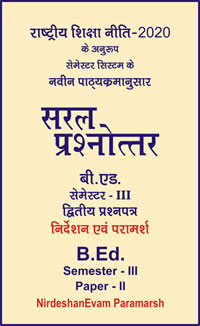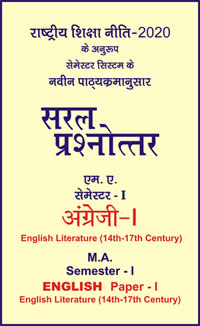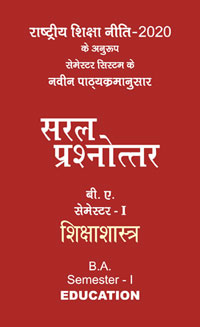|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- समावेशी विद्यालय की क्या विशेषताएँ हैं? समावेशी विद्यालय का विकास करते समय आप किन बिंदुओं को ध्यान रखें?
उत्तर -
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने इस ओर विशेष बल दिया कि जहां तक संभव हो शारीरिक रूप से बाधित, दृष्टि-युवक, श्रवण और अन्य असमर्थ बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ होनी चाहिए। केवल गम्भीर रूप से दृष्टि-प्रत्यर, बाधित या अंगहीन के लिए विशेष शिक्षा संस्थानों में प्रवेश की व्यवस्था की जाए। कौटारी आयोग ने समानित शिक्षा की सिफारिश की थी। इन विशेष बालकों की शिक्षा को मुख्य धारा में सम्मिलित करने के परिणाम स्वरूप विशेष शिक्षा का विकास हुआ। इस विकास के चलते विशेष शिक्षा पृष्ठभूमिकरण में समावेशी शिक्षा की और असर हुआ।
समावेशी शिक्षा के अंतर्गत एक आदर्श समावेशी विद्यालय की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं -
- समस्त विद्यालय के शिक्षण एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों द्वारा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को पूर्ण सहयोग के साथ समान रूप से निभाया जाना।
- विशेष आवश्यकता वाले बालक-बालिकाओं को भी कक्षा में सामान्य बालकों की तरह कक्षा से जो शिक्षण ग्रहण करते हैं उनका पालन करेंगे।
- समावेशी विद्यालय के सभी विद्यार्थियों को आवश्यकतानुसार राज्य एवं निजी मूल्यांकन में आवश्यक अथवा स्वीकृत संशोधन के साथ भाग लेना।
- सभी शिक्षण कर्मचारियों के सदस्यों द्वारा स्कूल के विकास हेतु योजनाओं के निर्माण में हिस्सा लेना व सहयोग देना।
- सभी विद्यार्थियों को साधारण विद्यार्थियों की तरह व्यवहार करना।
- समावेशी बच्चों के विकास के लिए शिक्षण एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किया जाना।
- समावेशी विद्यालय सभी अभिभावकों विशेषकर दिव्यांग बालकों के अभिभावकों को विद्यालय की सभी आवश्यक गतिविधियों में सम्मिलित करना।
- समावेशी विद्यालय के स्टाफ द्वारा समावेशी बालकों के साथ निरंतर संवाद करते रहना।
- समावेशी बालकों की आवश्यकताओं एवं सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए विद्यालय में आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित किया जाना।
- स्कूल कर्मचारियों द्वारा एक-दूसरे के लिए संसाधनों के रूप में सेवा देने के लिए तत्पर रहना।
- स्कूल प्रबंधन तथा प्रशासन द्वारा स्वयं समावेशी विद्यालय के लिए आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता पर नजर रखना एवं उनका समावेशी बालकों के लिए उपयोग किए जाने के प्रति निरंतर जागरूक रहना।
समावेशी विद्यालय विकास के बिंदु
एक आदर्श समावेशी विद्यालय में प्रायः यह देखा जाता है कि कुछ दिव्यांग बालकों की गंभीरता व उनकी असमर्थता इतनी गंभीर होती है कि वे सामान्य बालकों के साथ शिक्षा की दृष्टि से लाभान्वित नहीं हो सकते हैं। अतः ऐसे बालकों के लिए विशेष / समावेशी विद्यालय की व्यवस्था की जाती है क्योंकि सामान्य विद्यालयों में दिव्यांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था से सम्बंधित आवश्यक संसाधन व प्रशिक्षित शिक्षकों एवं शिक्षोत्तर कर्मचारियों की उपलब्धता न होने के कारण उनके मानसिक व शैक्षिक विकास को समझ नहीं हो पाती। यदि समावेशी विद्यालयों के द्वारा समावेशी शिक्षा की अवधारणा के साथ अपनाया जाए, तो यह आवश्यक है कि दिव्यांग बालकों को मुख्य धारा में लाया जा सकता हो। इसके लिए समावेशी विद्यालयों की स्थापना करते समय निम्नलिखित बिंदुओं को ध्यान में रखा जाना आवश्यक है -
-
विद्यालय का वातावरण - समावेशी विद्यालय भौतिक विद्यालय से अलग आवश्यकताओं को लेते हैं, अतः इसका वातावरण पूर्ण शिक्षकों, शिक्षोत्तर कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों के द्वारा निर्मित होता है, जो अनुकूल बनाए जाने की आवश्यकता होती है। सभी अपनी-अपनी जिम्मेदारी को जवाबदारी तरीके से निभाने का प्रयास करते हैं। आपस में सहयोग, सद्भाव व सामंजस्य की भावना के साथ कार्य व व्यवहार करें।
-
प्रशिक्षित स्टाफ - समावेशी विद्यालयों में कार्यरत समस्त स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। सामान्य विद्यालयों से इसमें प्राथमिकता होने के कारण इसके कार्मिकों को विशेष रूप से प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता होती है।
-
कक्षा-कक्ष प्रबंधन - प्रबंधन एक ऐसी सांगठनात्मक क्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के आधार पर विभिन्न कार्य किए जाते हैं जिनके परिणामस्वरूप विभिन्न मूल्यों, जैसे - मानवीय सम्मान, बैज्ञानिक एकता, स्व-अनुशासन तथा समूह संपत्ति का समावेशी होता है। कक्षा-कक्ष प्रबंधन के माध्यम से शिक्षण प्रक्रिया को सांगठित किया जाता है। इसप्रकार से अध्यापक के अध्यापन को निर्देशात्मक रूप और प्रभावशाली रूप दिया जाता है। इसके माध्यम से अध्यापन तथा विद्यार्थियों में रचनात्मक अधिगम के प्रति जागरूकता व प्रेरणा उत्पन्न करता है। अधिगम को प्रभावशाली बना सकते तथा विद्यार्थियों को सामाजिक, बौद्धिक व नैतिक विकास में सहयोग प्रदान किया जा सकता है। शिक्षकों में यह कार्य क्षमता होती है कि कक्षा-कक्ष प्रबंधन के कार्यों, क्रिया-कलाओं तथा कक्षा शिक्षण में सहायता की जा सकती है।
कक्षा-कक्ष प्रबंधन मुख्य रूप से शिक्षा से जुड़ा विषय है। इसमें अध्यापक की क्रियाएँ जैसे - अनुशासन, नियंत्रण, निष्कल आदेश, अभिप्रेरणा तथा अधिगम के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण सम्मिलित होते हैं। इस अभिनव वातावरण के निर्माण में अध्यापक की भूमिका केंद्रीय होती है। अध्यापक के कक्षा प्रबंधन की प्रणाली विशेषकर प्रविधियां जिन्हें अध्यापक कक्षा में उत्पादक तथा स्वतन्त्र क्रियाओं के कलाओं हेतु प्रयुक्त करता है, कक्षा प्रबंधन के मुख्य निर्धारक घटक हैं।
4. कक्षा-कक्ष प्रबंधन के महत्वपूर्ण नियम/अधिनियम व सिद्धांत - यह निम्नलिखित हैं -
- जब विद्यार्थी कक्षा के नियमों को भली भांति समझ लें तथा इन्हें स्वीकार कर लें तो वह उनका अनुसरण भी करें।
- कक्षा-प्रबंधन में केवल नियंत्रण पर ही बल न दिया जाये बल्कि इस बिंदु पर भी ध्यान दिया जाये कि विद्यार्थी अधिक से अधिक समय उत्पादक क्रिया-कलाओं में व्यतीत करें।
- विद्यार्थियों में बाह्य नियंत्रण के साथ-साथ आंतरिक नियंत्रण का विकास करना भी अध्यापक का लक्ष्य होना चाहिए।
- विद्यार्थियों को उनकी रुचि तथा योग्यताओं के अनुसार अर्थपूर्ण कार्यों में संलग्न रखने से अनुशासनहीनता की समस्या से निजात मिल सकती है।
- अति आवश्यक होने पर ही नियमों को बनाया जाए तथा स्पष्ट नियम ही बनाए।
- कक्षा की गतिविधियों में विलंब अथवा कम से कम हो।
- व्यक्तिगत पाठ तथा स्वतंत्र क्रियाओं का नियंत्रण।
- विद्यार्थियों को उत्तरदायित्व की भावना को महसूस करने के अवसर उपलब्ध कराना।
- विद्यार्थियों द्वारा उनकी क्षमता के अनुरूप किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित देना।
- पुनरवलोकन एवं उपयुक्त व्यवहार का प्रयोग करना।
5. समावेशी विद्यालय हेतु संसाधन प्रबंधन - समावेशी विद्यालय के लिए आवश्यक संसाधनों की उपलब्धता व प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु हैं -
- शिक्षण-अधिगम हेतु आवश्यक सामग्री की उपलब्धता एवं उनके रख-रखाव की सुव्यवस्थित व्यवस्था।
- कक्षा-कक्ष में पर्याप्त प्रकाश, हवा, ध्वनिरहित व साज-सज्जा की व्यवस्था।
- सामान्य फर्नीचर व विशेष फर्नीचर की उपलब्धता, उपयोग व रख-रखाव की व्यवस्था का निरीक्षण।
- एकीकृत क्रिया-कलाओं को करने के लिए पर्याप्त स्थान व खेल के मैदान की व्यवस्था तथा खेल उपकरणों की उपलब्धता।
- शैक्षिकउद्देश्यों के अनुसार बैठने व्यवस्था।
- सृजनात्मकता, निर्भरता, अनुसंधान, पर्यवेक्षण अभ्यास, शैक्षिक तकनीक व व्यवस्थित अभिनव प्रक्रियाओं का सुव्यवस्थित प्रबंधन।
- शैक्षिक तकनीक के अंतर्गत व्यवहार अनुसंधानात्मक प्रविधियां, व्यवहार परिवर्तन सम्बंधित प्रक्रिया उपकरण में सूचना तकनीक, प्रेस एवं अधिगम संसाधन प्रक्रिया को सम्मिलित किया जाता।
- शैक्षिक तकनीकों एवं उपकरणों की विद्यालय में उपलब्धता व उपयोग।
- सामान्य शारीरिक तथा वार्षिक क्रियाकलापों के नियोजन हेतु एक कैलेंडर का निर्माण व अनुश्रवण।
6. पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन - समावेशी विद्यार्थियों के विकास के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विशेष महत्व होता है। यह क्रियाएँ पाठ्यक्रम से अलग न होकर बालक पाठ्यक्रम का अटूट भाग हैं। इसलिए इसे पाठ्य सहगामी या पाठ्यत्तर क्रियाएँ कहा जाता है। सामान्य बालकों की तरह ही इन समावेशी बालकों को भी इनमें भाग लेने की अनुमति उपलब्ध रहती है। इन समावेशी बालकों को उनकी असमर्थता को ध्यान में रखते हुए ऐसी गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना व अवसर उपलब्ध कराना जिससे उनकी क्षमताओं का विकास हो सके व उनके मानसिक तनाव को कम किया जा सके।
|
|||||

 i
i