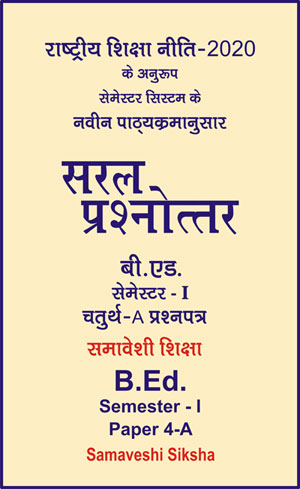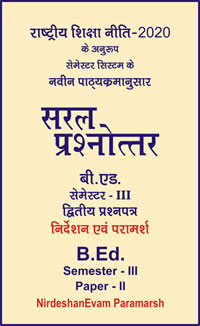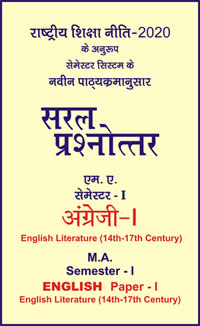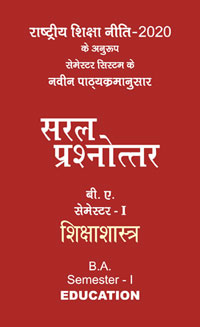|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- शिक्षण रणनीतियाँ क्या हैं? समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण क्षमताओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर -
शिक्षण रणनीतियाँ
(Pedagogical Strategies)
शिक्षण रणनीतियाँ वे ऐसी तकनीकें हैं जो प्रभावशाली शिक्षण में लागू की जा सकती हैं, जैसे - एक व्यापक पढ़ने की योजना। शिक्षण उद्देश्यों के लिए एक प्रभावी व सामयिक उद्देश्यों स्थापित किया जाता है। शिक्षण रणनीतियों का अवबोधन का अर्थ है सीखने के उद्देश्यों की उपलब्धि प्राप्त करने के लिए, एक नियोजित तरीके से शिक्षण शिक्षण कार्यक्रमों को चलाना।
विशेष रूप से, शैक्षिक रणनीतियों में एक प्रक्रिया या शिक्षण प्रणाली के शिक्षकों द्वारा विकास शामिल है, जिनमें मुख्य विशेषताएं यह हैं कि यह एक संगठित और औपचारिक कार्यक्रम का गठन करती है और यह विशिष्ट और पहले स्थापित उद्देश्यों की उपलब्धि के लिए उपयुक्त या प्रयुक्त होता है।
समावेशी शिक्षा के लिए आवश्यक शिक्षण क्षमताएँ
समावेशी विद्यालय में शिक्षक के कुछ आवश्यक क्षमताएँ होनी चाहिए ताकि वे अपनी क्षमताओं का उपयोग कक्षा शिक्षक के रूप में छात्रों को ज्ञान देने में सक्षम हो सकें। इन विशेष शिक्षण क्षमताओं का वर्णन इस प्रकार है -
1. समावेशी शिक्षण का प्रयोग - शिक्षक को बालकों की वैयक्तिक विशेषताओं का ज्ञान हो साथ ही विशेष आवश्यकता वाले बालकों को पहचान कर उनके अनुसार कक्षा शिक्षण को अनुकूलित करने में सक्षम होना चाहिए। उदाहरणस्वरूप, धीमी गति से सीखने वाले विशेष छात्र यदि कक्षा शिक्षण में पिछड़ गए हों तो उनके लिए विशेष कक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।
समावेशी शिक्षण में रणनीतियों का उपयोग आवश्यक होता है। उनका कब, कहाँ, कैसे, कितना प्रभावी रूप से उपयोग किया जाए यह भी सुनिश्चित होना चाहिए। शिक्षक को कक्षा में छात्रों के मानसिक स्तर व अनुकूल उपयुक्त शिक्षणसामग्री, सहायक शिक्षण सामग्री तथा शिक्षण विधियों का प्रयोग करना चाहिए।
2. शिक्षण में लचीलापन - शिक्षण क्षमताओं में लचीलापन का गुण होना चाहिए। कक्षा के स्तर, बालकों की रुचि, विषय-वस्तु की जटिलता, बालकों की वैयक्तिक विभिन्न विशेष समस्याओं को दृष्टि में रखते हुए लचीला शिक्षण होना चाहिए। जब शिक्षक को छात्रों से प्रश्न करने आदि के दौरान ऐसा लगे कि छात्र समझ नहीं पाए हैं, तो उसे अपनी शिक्षण विधि में बदलाव कर लेना चाहिए। विशेष बालकों से अंतःक्रिया कर शिक्षक को पता लगाना चाहिए कि छात्र कितना सीख पा रहे हैं, तो उनके अनुकूल दृश्य-श्रव्य साधन, सहायक सामग्री आदि का प्रयोग कर विषय को उनके लिए सहज व बोधगम्य किया जा सकता है।
3. क्रियात्मक शिक्षण - कक्षा शिक्षण में मूर्तिकरण, व्याख्या प्रणाली, प्रश्नोत्तर कला आदि के अभ्यास से त्वरित व क्रियात्मक शिक्षण प्रभावशाली शिक्षण सिद्ध होता है। क्रियात्मक शिक्षण में श्रवणेंद्रिय, दृष्टेंद्रिय के साथ क्रियात्मक भी सम्मिलित हो जाने पर पाठ्य सहगामी सहज बोधगम्य हो जाता है। यह उसी प्रकार है जैसे स्कूल चलाना या तैराकी में तरना। हम पढ़कर नहीं समझ सकते, परंतु स्कूटर चलाना या तैराकी में तैरते हुए हम अधिक प्रभावी ढंग से सीखते हैं। प्रयोगशालाओं में विज्ञान के प्रयोग उस विषयक ज्ञान प्राप्त करने में अधिक प्रभावी होते हैं क्योंकि इनमें क्रियात्मकता सम्मिलित है। युक्त वैज्ञानिक शिक्षण विद्यार्थियों को बाह्यजगत बनाते हैं जबकि अवबोधन उसे रुचिकर बनाते हैं।
4. सहायक शिक्षण सामग्री का प्रयोग - चित्र, चार्ट, दृश्य-श्रव्य साधन, टेलीविजन, वीडियो, फिल्म, प्रोजेक्टर आदि का शिक्षण में उपयोग इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत पर आधारित है कि जिस शिक्षण में ज्ञानेंद्रियों का जितना अधिक उपयोग होगा, वह उतना बोधगम्य होगा। दृश्य-श्रव्य साधन कान के अतिरिक्त आंख तथा मस्तिष्क को चेतन में सम्मिलित कर अधिक शिक्षण सामग्री आकर्षक तथा रुचिकर हो जाते हैं। त्रियामी (3D) वस्तुएं मंदबुद्धि वाले बालकों हेतु भी शिक्षण में प्रमुख व प्रभावशाली रहती हैं। समावेशी शिक्षण में शिक्षण सामग्रियों का उपयोग विशेष तथा सामान्य दोनों प्रकार के छात्रों के लिए उपयुक्त है।
5. विभिन्न शिक्षण योजनाओं का उपयोग - समावेशी शिक्षा में शिक्षण व्यवस्था का निर्माण करना यह उसी प्रकार निर्धारित करना होता है कि कब, कहाँ, कैसी शिक्षण विधियों का रणनीति अपनाई जाएगी जैसे युद्ध के समय सैनिकों द्वारा योजना बनाकर कार्य किया जाता है। शिक्षाविद् डॉ. के. सी. पाण्डेय यह कहते हैं कि, "शिक्षण से पूर्व की अवस्था में भी तैयारी का समावेश एक प्रमुख परिणाम होता है कि शिक्षक के सामने एक सुनिश्चित योजना तैयार हो जाती है।" इस प्रकार से शिक्षण को अधिक प्रभावी व शिक्षण प्रक्रिया करने के लिए अपने को सक्षम बनाया जा सकता है।
शिक्षण की पूर्व तैयारी उतनी ही महत्वपूर्ण रखनी है जितना गुफाओं में प्रवेश करने से पहले मशालों का उपलब्ध रहना, रणनीति, आवश्यक उपकरणों व आयु का ध्यान रखना। विभिन्न प्रकार की शिक्षण विधियों का प्रयोग समावेशी शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। प्रमुख शिक्षण विधियाँ - योजना विधि (प्रोजेक्ट मैथड), समस्या समाधान विधि, पैटर्न अवबोधन शिक्षण, डायलॉग पद्धति, आनंदम व निगमन विधि आदि।
6. वैयक्तिक शैक्षिक कार्यक्रम (I.E.P.) - निशक्त बालकों हेतु I.E.P. अर्थात् इंडिविजुअल एजुकेशन प्रोग्राम एक उपकरण है जो बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं, बालक के वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति को गई सेवाओं तथा कार्यक्रमों को प्रभावशाली व विशिष्ट बनाता है। I.E.P. का मान्यता है कि विभिन्न निशक्त बालकों की शैक्षिक आवश्यकताओं को उचित व्यावसायिक शैक्षिक आवश्यकताओं का निर्माण कर प्रदान किया जाए। समावेशी शिक्षा में निर्मित कक्षा-कक्ष में विशेष बालकों के शिक्षण व पाठ्यक्रम के समायोजन के लिए I.E.P. प्रभावी भूमिका निभाता है। स्तर को धीमा करने के स्थान पर दृश्य तथा मौखिक दोनों स्तर पर शिक्षण प्रदान किया जाना चाहिए।
7. अंतःक्रियात्मक शिक्षण - शिक्षक को केवल व्याख्यान या भाषण देकर ही अपने शिक्षण को पूर्ण समझना एकतरफा मार्ग है—अर्थात् शिक्षक जितना सक्रिय हो बालकों को भी उतना ही सक्रिय होना चाहिए। प्रश्नोत्तर अंतःक्रियात्मक शिक्षण का प्रभावी उपाय है। प्रश्न एक ही विद्यार्थी ने न पूछकर समान रूप से पूछे जाने चाहिए। अंतःक्रियात्मक शिक्षण को स्पष्ट करते हुए पी. डब्ल्यू. जैक्सन ने लिखा है—"शिक्षक विद्यार्थियों को अनेक प्रकार की शाब्दिक एवं अशाब्दिक प्रेरणाएँ देता है; प्रश्न पूछता है; विद्यार्थियों के उत्तर सुनता है और उनका मूल्यांकन करता है।" इस सिद्धांत (शिक्षक, पाठ्य, छात्र) अंतःक्रिया में विशेष तथा सामान्य दोनों प्रकार के बालकों को सम्मिलित कर प्रभावी शिक्षण किया जा सकता है।
8. प्रबलन या पुनर्बलन (Reinforcement) - कक्षा शिक्षण में शिक्षण पुनर्बलन का प्रयोग शिक्षण में सफलता प्राप्त करने के लिए शिक्षक द्वारा किया जाता है। यदि उत्तर सही है तो शिक्षक सही उत्तर देने वाले छात्र पर प्रसन्न होकर उसे शाबाशी देता है। यदि उत्तर कुछ-कुछ सही है, अतः कुछ नहीं कहने से शिक्षक छात्र को प्रोत्साहित करता है। इस तरह कक्षा शिक्षण में पुनर्बलन द्वारा छात्रों को उत्तेजित करने का प्रयास किया जाता है। शिक्षण हाँ, अच्छा, चालाक आदि कहकर या उत्तर ठीक होने पर प्रसन्नता से सिर हिलाकर, मुस्कुराकर या हाथ के संकेत से छात्रों को पुनर्बलन करता है। समावेशी शिक्षा में सामान्य व विशेष दोनों प्रकार के छात्रों के लिए पुनर्बलन उन्हें सीखने में सहायता करता है।
9. शिक्षण कौशल, शिक्षण सूत्रों का प्रयोग - शिक्षण की क्षमताओं से युक्त करने के लिए शिक्षक को उन शिक्षण कौशलों तथा शिक्षण सूत्रों को आवश्यकतानुसार प्रयोग में लाना चाहिए। प्रमुख शिक्षण कौशल हैं—पाठ प्रस्तुतीकरण कौशल, उद्देश्य कथन कौशल, अनुशासन कौशल, प्रश्न महत्वपूर्ण कौशल, श्यामपट्ट कार्य कौशल, पाठ समापन कौशल आदि। प्रमुख शिक्षण सूत्र हैं—सरल से कठिन की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, संकल्पना से विवरण की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर इत्यादि। समावेशी शिक्षा में इनका उपयोग विषय सामग्री को अवबोध व बनाकर सुगम्य बनाता है।
10. पाठ योजना तैयार कर शिक्षण - किसी भी कार्य को करने से पूर्व, यदि उसकी योजना बना ली जाए तो कार्य निर्विघ्न हो जाता है तथा उसकी सफलता की संभावना बढ़ जाती है। शिक्षण को क्षमतायुक्त बनाने हेतु शिक्षक को विषय-वस्तु को छोटी-छोटी इकाइयों में विभाजित करके अध्यापन की योजना बनानी चाहिए। कमजोर बालकों हेतु शिक्षण की विधि का एवं इसे पूर्व निर्धारित किया जाना चाहिए ताकि सामान्य शिक्षण में सहायक सामग्री के साथ वह कब प्रदर्शित की जाएगी। इसका पाठ योजना में प्रावधान होना चाहिए। प्रस्तुतिकरण को प्रभावशाली बनाने हेतु अध्यापक सबसे पहले पूछे जाने वाले विकास प्रश्न, बोध प्रश्न को प्रस्तुत करने के लिए योजना बनाए। इस तरह से पुनर्बलन प्रक्रिया तथा कक्षा अध्ययन व गृहकार्य को जोड़ते हुए पाठ योजना बनाई जाए जिससे समावेशी शिक्षण सामान्य व विशेष दोनों प्रकार के बालकों के अधिगम तथा शिक्षण को बोधगम्य हेतु उपयुक्त हो।
|
|||||

 i
i