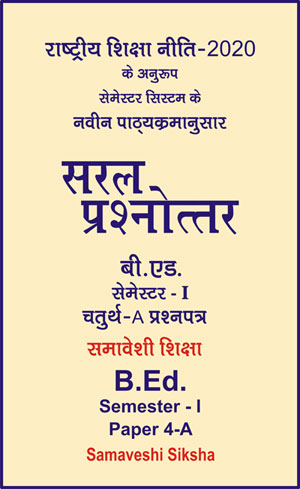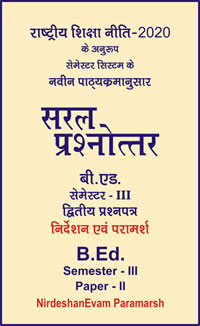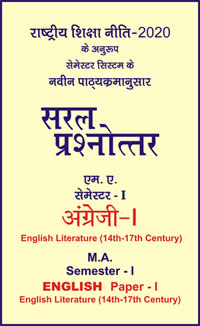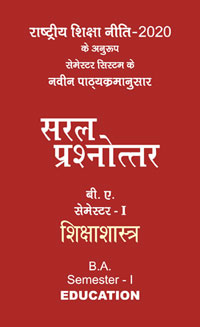|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- श्रवण बाधिता तथा असमर्थता का क्या अर्थ है? शैक्षणिक एवं विशेषताओं, कारणों, पहचान तथा देखभाल एवं प्रशिक्षण का वर्णन कीजिए।
अथवा
आप ‘श्रवण बाधित’ बालकों की पहचान किस प्रकार कर सकते हैं? इनकी विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं की सुविधाओं का विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिए।
अथवा
श्रवण अंगभंग की परिभाषा दीजिए। समावेशी स्कूलों में ऐसे बालकों के लिए क्या-क्या शैक्षिक प्रावधान बनाए जा सकते हैं? वर्णन कीजिए।
अथवा
‘श्रवण बाधिता’ को परिभाषित कीजिए। अपनी कक्षा में ऐसे बच्चों की पहचान आप कैसे करेंगे, स्पष्ट कीजिए।
उत्तर-
श्रवण बाधित और असमर्थता का अर्थ -
श्रवण बाधिता का सम्बन्ध श्रवण यंत्र प्रक्रिया के क्षतिग्रस्त होने से है। यह क्षति कान के किसी भी भाग में हो सकती है, जैसे बाहरी, मध्य या आंतरिक अंगों में। इसी श्रवण बाधिता से श्रवण असमर्थता उत्पन्न होती है। यह श्रवण असमर्थता न्यूनतम से अधिकतम हो सकती है। व्यक्ति पूर्ण रूप से बहरा या ऊँचा सुनने वाला हो सकता है। यह दोष बालकों की प्रकृति और श्रवण-दोष की मात्रा पर निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति या बच्चा जन्म से ही श्रवण प्रक्रिया में बाधित हो सकता है या फिर जन्म के परवश चोट, संक्रमण या दुर्घटना के कारण हो सकता है।
श्रवण बाधित तथा असमर्थ बच्चों की विशिष्टताएँ-
श्रवण बाधित एवं असमर्थ बच्चों या व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं का अध्ययन निम्नलिखित श्रेणियों के अनुसार किया जा सकता है—
- भाषा और वाणी का विकास
- बौद्धिक योग्यता
- शैक्षिक उपलब्धि
- सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन
- कुछ अन्य विशेषताए
1. भाषा और वाणी का विकास-
भाषा और वाणी के विकास से जुड़ी निम्न विशेषताएँ श्रवण असमर्थ लोगों में होती हैं—
(i) बिना प्रशिक्षण के श्रवण असमर्थ बालकों में भाषा का विकास सामान्य नहीं होता।
(ii) श्रवण बाधित और असमर्थ बच्चों में भाषा सीखने की योग्यता कमजोर होती है।
(iii) बहरेपन से बोलने में अयोग्यता स्वयं ही आ जाती है।
(iv) श्रवण दोष जितना प्रारम्भ में होगा, भाषा की कमी उतनी अधिक होगी।
(v) जबकि अत्यधिक श्रवण दोष सामान्य भाषा विकास में बाधक होता है, फिर भी कुछ ऐसे बहरे होते हैं जिन्हें भाषा का कुछ प्रयोग नहीं सिखाया जा सकता।
2. बौद्धिक योग्यता-
बौद्धिक योग्यता से जुड़ी असमर्थ व्यक्तियों की विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं—
(i) यह आवश्यक नहीं होता कि बहरे बच्चे सामान्यों की तुलना में बौद्धिक विकास में धीमे ही हों।
(ii) सामान्य और बहरे बच्चों में चिंतन प्रक्रिया एक समान ही होती है।
(iii) बहरे बच्चे सामान्य बच्चों की तुलना में बौद्धिक क्रियाओं में कार्य सम्पन्नता का कम प्रदर्शन करते हैं।
(iv) श्रवण बाधित बच्चों के असांगठित बुद्धि परीक्षणों में शाब्दिक परीक्षणों के अपेक्षा अधिक अंक होते हैं।
3. शैक्षिक उपलब्धि-
शैक्षिक उपलब्धि के क्षेत्र में असमर्थ बच्चों की विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं-
(i) श्रवण बाधित व असमर्थ बच्चों की शैक्षिक उपलब्धियों के क्षेत्र में कमी रहती है।
(ii) इन बच्चों में पढ़ने सम्बन्धी न्यूनता होती है जो कि भाषा कौशलों पर निर्भर करती है।
(iii) श्रवण बाधित या असमर्थ बच्चों को शैक्षिक उपलब्धि के निर्देशात्मक चित्र में कोई सुधार दिखाई नहीं देता।
(iv) ऐसे बच्चों को शैक्षिक उपलब्धि में न्यूनतम का मुख्य कारण होता है - स्कूल और कक्षा का वातावरण जिसकी प्रकृति भाषायी होती है और बहरे बच्चों में भाषा-कौशलों का अभाव होता है।
4. सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन-
सामाजिक और व्यावसायिक समायोजन सम्बन्धी विशेषताएँ निम्नलिखित होती हैं-
(i) श्रवण बाधित बच्चों की सामाजिक और व्यक्तिगत विशेषताएँ सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत भिन्न होती हैं।
(ii) ऐसे बच्चे, संप्रेषण समस्याओं और सामाजिक अंतःक्रिया में असफलता के कारण अलग-थलग रहते हैं।
(iii) श्रवण बाधित बच्चे अलग एक समूह बना लेते हैं, जिसमें इनकी रुचियाँ सीमित होती हैं।
(iv) ऐसे बच्चों में संप्रेषण समस्या के कारण सामाजिक समायोजन की समस्या भी बहुत गंभीर होती है।
(v) ऐसे बच्चों में सामाजिक अंतःक्रिया और सामाजिक स्वीकृति की इच्छा बहुत सराहनीय होती है।
(vi) श्रवण बाधित बच्चे संपृक्तात्मक-समायोजन की दृष्टि से सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं।
5. कुछ अन्य विशेषताएँ-
अध्ययनों ने श्रवण बाधित व असमर्थ बच्चों की कुछ अन्य विशेषताओं को बताया है, जैसे-
(i) श्रवण-बाधित बच्चे बौद्धिक योग्य, शैक्षिक उपलब्धि और वैयक्तिक-सामाजिक समायोजन की दृष्टि से निम्न स्तर के होते हैं।
(ii) ऐसे बच्चे IQ परीक्षणों में अपेक्षाकृत कम अंक लेते हैं।
(iii) शैक्षिक विषयों में इनकी कार्य-सम्पन्नता निम्न स्तर की होती है।
(iv) ये सभी न्यूनतम मूलभूत भाषायी कौशलों के विकास के अभाव के परिणामस्वरूप कमजोर होते हैं।
यह आवश्यक नहीं कि उपरोक्त सभी विशेषताएँ हर एक असमर्थ में विद्यमान हों। हर श्रवण असमर्थ बालक इन विशेषताओं की दृष्टि से एक-दूसरे से भिन्न हो सकता है।
श्रवण असमर्थता के कारण- श्रवण असमर्थता के कारण लोगों को जानना भी अति आवश्यक है। यह ज्ञान इन दोषों का सामना करने और बच्चों की सहायता करने में सहायक हो सकता है। इसके विभिन्न कारण हो सकते हैं, जो निम्नलिखित हैं-
1. जन्म के समय तथा जन्म के बाद की परिस्थितियाँ- जन्म के समय तथा जन्म के परवश विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ बच्चों में इस प्रकार की असमर्थता के लिए उत्तरदायी हो सकती हैं। जैसे, जन्म के समय प्रयोग किये गए उपकरण, रोगों से ग्रस्त आदि लगना, ऑक्सीजन का अभाव, आदि। इसी कारण बच्चे के जन्म के एकदम बाद बच्चे को पीलिया (श्वसनकष्ट) हो जाना, कान या आँख से किसी द्रव पदार्थ का बहना आदि इन दोषों को तुरंत दूर किया न जाये तो यह दोष श्रवण-बाधिता पैदा कर देते हैं।
2. वंशानुगत- कई बार यह दोष एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित हो जाता है। अर्थात् यह वंशानुगत भी हो सकता है।
3. कुपोषण- बच्चों का कुपोषण भी कई बार श्रवण बाधिता के लिए उत्तरदायी होता है। जैसे, गर्भावस्था के दौरान यदि माँ को संतुलित आहार न मिले तो इन दोषों की संभावना रहती है। यदि गर्भावस्था में माँ तीखे मसाले, शराब, सिगरेट आदि का सेवन करती है तो भी इन दोषों के पनपने की पूरी संभावना रहती है। अतः गर्भावस्था में माँ को कुपोषण से बचना चाहिए।
4. छूत के रोग- बच्चा जब जन्म लेता है यदि वह छूत के रोगों का शिकार हो जाता है तो इससे उसकी श्रवण शक्ति प्रभावित होती है। परिणास्वरूप श्रवण क्षमता (Hearing capability) कुंठित हो जाती है। अतः नये पैदा हुए बच्चे को छूत के रोगों से बचाना चाहिए।
5. दवाएँ- कभी-कभी गर्भवती महिला का अत्यधिक दवाओं का सेवन भी श्रवण बाधिता का कारण बनता है। जैसे, गर्भावस्था के दौरान यदि किसी महिला को मलेरिया जैसे बुखार हो जाये और उसे रोकने जैसे दवा दी जाए तो इसका प्रभाव गर्भ में पल रहे बच्चे के किसी न किसी अंग पर पड़ सकता है। गर्भवती महिलाओं को दवाओं के अधिक सेवन से बचना चाहिए।
श्रवण बाधितों या असमर्थों की पहचान- श्रवण बाधितों की शीघ्र पहचान करना अति आवश्यक होता है। इनकी पहचान में देरी करने से इनकी भाषा का विकास कुंठित होता है। परिणास्वरूप वे स्कूल भी छोड़ देते हैं। श्रवण बाधितों की पहचान के लिए चेक-लिस्ट का प्रयोग किया जा सकता है-
(i) क्या बच्चा चेवानी का प्रदर्शन करता है?
(ii) क्या बच्चे के कान में कोई विकृति है?
(iii) क्या बच्चे के कान से कोई तरल पदार्थ बहता है?
(iv) क्या बच्चा निर्देशों की पुनरावृत्ति के लिए कहता है?
(v) क्या बच्चा कान में बार-बार दर्द की शिकायत करता है?
(vi) क्या बच्चा आपके निर्देशों को पहचान करने में असमर्थ है?
(vii) क्या बच्चा अपने कान में बार-बार खुजली करता है?
(viii) क्या बच्चा बोलते समय व्यक्ति के चेहरे स्वयं को केंद्रित करता है?
(ix) कक्षा में जब अध्यापक मौखिक रूप से कुछ समझाता है तो क्या बच्चा अपने साथियों से नोट लेने के लिए सहायता मांगता है?
उपरोक्त प्रश्नों के यदि कुछ उत्तर 'हाँ' हैं तो अध्यापक बच्चे की श्रवण-बाधिता का परीक्षण करवा सकता है। अनुमान लगा सकता है। ऐसे बच्चे को विशेषज्ञ के पास तुरंत भेज देना चाहिए। यदि जाँच की रिपोर्ट मध्यम स्तर की श्रवण-बाधिता बताती है तो उसे नियमित स्कूल में भेजना चाहिए। यदि जाँच रिपोर्ट बहुत अधिक दोष बताती है तो उसे बहरे के स्कूल में भेजना चाहिए।
श्रवण बाधित बालकों की शिक्षा के लिए प्रमुख व्यवस्थाएं/रणनीतियाँ
श्रवण असमर्थ बालकों की देखभाल और प्रशिक्षण- श्रवण असमर्थ बालक एक-दूसरे से भिन्न होते हैं। यह भिन्नता श्रवण दोष के प्रकार और मात्रा के रूप में होती है।
शिक्षा का अधिकार हर व्यक्ति को है चाहे वह समर्थ हो या असमर्थ हो। इनकी देखभाल और प्रशिक्षण सभी का उत्तरदायित्व होना चाहिए जैसे परिवार, स्कूल, समाज, स्वास्थ्य तथा समाज-कल्याण से जुड़े व्यक्तियों का इन उत्तरदायित्वों का वर्णन इस प्रकार है—
1. माता-पिता का उत्तरदायित्व- श्रवण बाधित बालक की देखभाल और प्रशिक्षण घर से माता-पिता, भाई-बहनों, तथा परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा शुरू होनी चाहिए। इसका इस संदर्भ में उत्तरदायित्व निम्नलिखित है—
(i) आवाज और वाणी के प्रति अनुक्रियाओं परखाधारित बच्चे की शीघ्रता पहचान करना।
(ii) जाँच के लिए श्रवण वाले कानों को ENT और आँखों के विशेषज्ञों के पास भेजना।
(iii) परिवार द्वारा श्रवण-असमर्थ बच्चे को प्रति प्रेम का प्रदर्शन करना तथा अन्य सामान्य बच्चों जैसा स्नेह देना।
(iv) ऐसे बच्चों के प्रशिक्षण के लिए अध्यापकों और विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करना।
(v) श्रवण-सहायता के नियमित प्रयोग के लिए बच्चे को प्रोत्साहित करना।
(vi) विशेषज्ञों की सलाह का अनुसरण करना।
(vii) स्कूल में एकीकरण के लिए बच्चे को तैयार करना।
(viii) बच्चे की घर एवं सामाजिक सामान्यता हेतु परिस्थितियों को उत्पन्न करना।
2. स्कूल का उत्तरदायित्व- माता-पिता के अतिरिक्त स्कूल का भी बच्चों को देखभाल और प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायित्व होता है। इन बच्चों की मुख्य समस्या इनकी बहरे बच्चों के प्रशिक्षण की तीन विधियाँ होती हैं—
(a) शाब्दिक विधि
(b) मैनुअल विधि
(c) सम्पूर्ण संप्रेषण उपागम
(a) शाब्दिक विधि- जैसे सुनने या प्रशिक्षण होने का पढ़ना या स्पीच पढ़ना आदि सभी शाब्दिक विधि के उदाहरण हैं।
(b) मैनुअल विधि- यह विधि अत्यधिक बहरे बच्चों के लिए उपयुक्त है। इस विधि के उदाहरण हैं— संकेत भाषा और फिंगर स्पेलिंग।
(i) संकेत भाषा- प्रभावशाली संप्रेषण ही श्रवण असमर्थ बच्चों की मुख्य समस्या होती है। इस पर नियंत्रण पाने के लिए अधिकांश लोग संकेत भाषा का प्रयोग करते हैं। यह भाषा सामान्य भावों को समझाने के लिए हावभावों की एक प्रणाली होती है। संकेतात्मक भाषाओं की बहुत-सी किस्में हैं।
आजकल अमेरिकी सांकेतिक भाषा ‘अमेरिसेलन’ का प्रयोग बढ़ा है। बहरे व्यक्ति और उनके परिवार के बच्चों को ऐसे बच्चों को प्रशिक्षण किया जाता है। यह केवल प्रशिक्षक प्रशिक्षण ही नहीं बल्कि जब कक्षा में पढ़ाते समय अध्यापक को इस सांकेतिक भाषा का प्रयोग अधिक से अधिक करना चाहिए।
(ii) फिंगर स्पेलिंग- जो अत्यधिक बहरे बच्चे स्कूल जाने का अनुभव रखते हैं उन्हें स्पेलिंग का ज्ञान दिया जा सकता है ताकि संप्रेषण में उन्हें सहूलियत मिल सके। इस विधि के अन्तर्गत हवा में उंगलियों द्वारा आकृतियाँ बनाकर लिखा जाता है। इसमें वे शब्द जिनके लिए कोई संकेत या चिन्ह नहीं होता, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, लिखा जाता है। इस प्रकार फिंगर स्पेलिंग व्यक्ति द्वारा लिखित भाषा का प्रदर्शन है। साधारण भाषा में हम कह सकते हैं कि यह अक्षरों को उंगलियों की स्थिति का प्रयोग करके समझाना होता है। कुछ सीमा तक यह छपे हुए अक्षरों से मेल खाता है।
भारत में दो प्रकार के फिंगर स्पेलिंग का प्रयोग किया जाता है। दोनों ही अंग्रेजी अक्षरों पर आधारित होते हैं। हर अक्षर (A to Z) का विशिष्ट आकार होता है। अमेरिकी प्रणाली के अन्तर्गत इसमें एक ही हाथ का प्रयोग किया जाता है जबकि ब्रिटिश प्रणाली में दोनों का प्रयोग होता है। भारतीय प्रणाली ‘करा अल्फ़बेट’ के नाम से भारतीय परिस्थितियों के लिए अमेरिका एक हाथ-प्रणाली पर आधारित इस विधि का विकास किया गया है।
(iii) स्पीच रीडिंग- स्पीच रीडिंग को कभी-कभी ‘लिप रीडिंग’ भी कहा जाता है। इसमें श्रवण बाधित व्यक्ति होठों की हलचल या मुँह की हलचल का अवलोकन करता है तथा यह समझने का प्रयास करता है कि बोलने वाला क्या बोल रहा है। स्पीच रीडिंग का मुख्य लक्ष्य है-
(a) वातावरण में दिखाई देने वाले उदाहरणों का अवलोकन करना।
(b) जो कुछ बोल रहा है उसे समझना।
(c) बोलने वाले होठों की हलचल और चेहरे के हावभावों का अवलोकन करना।
(iv) श्रवण प्रशिक्षण- बहरे बच्चों बार श्रवण बाधित बच्चों में कुछ सुनने की योग्यता होती है। इस थोड़ी-सी बची हुई (Residual) श्रवण क्षमता का प्रयोग करने के लिए इसे उचित प्रशिक्षण देना चाहिए। इस प्रशिक्षण के तीन लक्ष्य होते हैं-
(a) विभिन्न प्रकार की आवाज़ों का जागरूकता का विकास करना।
(b) वातावरणीय आवाज़ों में भेदकरण करने की योग्यता का विकास करना।
(v) सम्पूर्ण संप्रेषण विधि- यह नवीन विधि हाल ही में विकसित हुई है। इस विधि में सभी विधियों और साधनों का मिश्रण कर दिया जाता है। शाब्दिक या वैकल्पिक विधि सभी प्रकार के श्रवण बाधियों के लिए उपयुक्त नहीं हो सकती अतः यह सम्पूर्ण संप्रेषण विधि विभिन्न "टूल्स" में अधिक लाभदायक हो रही है।
(vi) पाठ्यक्रम और शिक्षण योजना रचना- श्रवण बाधित बच्चे सभी प्रकार के पाठ्यक्रम को नहीं समझ पाते सकते अतः हमें उनके लिए उनकी आवश्यकताओं और समस्याओं के अनुसार ही पाठ्यक्रम अपनाना चाहिए। इसके लिए निम्न सिद्धांत आवश्यक होते हैं-
(a) जब किसी पाठ्यक्रम को अपनाया जाता है तो निर्देशकों के लक्ष्य सामान्य और श्रवण असमर्थ बच्चों के लिए एक समान होने चाहिए। केवल सीखने की सामर्थ्य और विधियों में संशोधन इस प्रकार किया जाना चाहिए जिससे कक्षा में सामान्य बच्चों की शिक्षा की विलम्बता न किया जाये।
(b) कक्षा में भारत में श्रवण बाधित और सामान्य बच्चों का अनुपात 1:5 होना चाहिए। श्रवण बाधित बच्चों को कक्षा में आगे के बच्चों पर बिठाया जाना चाहिए। इससे उनको सुनने में सहायता मिलेगी।
(c) कक्षा में अध्यापक यह देखे कि श्रवण बाधित बच्चा अपनी सुनने की मशीन का नियमित प्रयोग कर रहा है या नहीं।
(d) ऐसे बच्चों का स्पीच और भाषा का पैटर्न पर्याप्त रूप से विकसित हो जाना चाहिए। श्रवण-बाधित बच्चों का भाषा सीखने और उसके प्रयोग का पैटर्न दोषपूर्ण होता है। वे आमतौर पर जैसे बोलते हैं, वैसा ही लिखते हैं।
(e) ऐसे बच्चे अमूर्त प्रश्नों को सोचने में कठिनाई का सामना करते हैं।
(f) ऐसे बच्चे स्पीच और भाषा सीखने में कठिनाई अनुभव करते हैं इसलिए वे अन्य विषयों को सीखने में भी कठिनाई महसूस करते हैं।
(g) अध्यापक को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि बच्चा क्या सुन सकता है, वह और क्या सुन सकता है तथा उसे बच्चे की शैक्षिक आवश्यकताओं के अनुसार पाठ योजना बनानी चाहिए।
|
|||||

 i
i