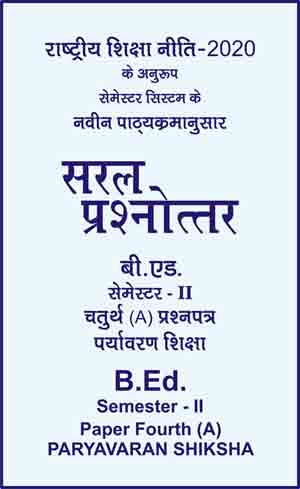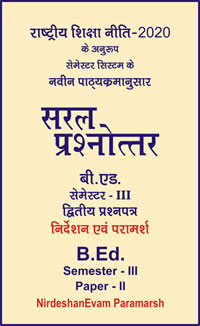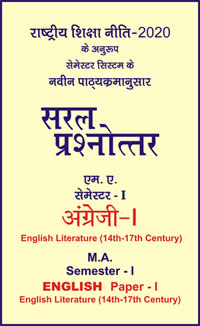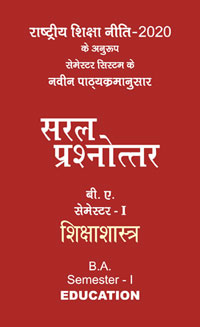|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षा बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
अध्याय - 3 पर्यावरणीय शिक्षा में विभिन्न आयाम
(Various Approaches in EnvironmentalEducation)
प्रश्न- पर्यावरण शिक्षा के पाठ्यक्रम को संक्षेप में समझाइए ।
अथवा
प्राथमिक एवं माध्यमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षा के पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालिए।
अथवा
विद्यालयी पाठ्यक्रम में पर्यावरणीय शिक्षा को सम्मिलित करने के अन्तर- अनुशासनिक एवं बहु- अनुशासनिक मॉडल का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
पर्यावरण शिक्षा का पाठ्यक्रम
पर्यावरण अध्ययन में सामाजिक अध्ययन आता है। सामाजिक अध्ययन के पठन द्वारा छात्र अपने आस-पड़ोस, प्रदेश तथा दूसरे देशों के रीति-रिवाज, रहन-सहन तथा संस्कृति के विषय में अध्ययन करते हैं। विभिन्न समाजसेवी संस्थायें एवं अभिकरण किस प्रकार हमारी सहायता करते हैं। हम किस प्रकार दूर संचार तथा यातायात के साधनों के विषय में पठन करते हैं।
पर्यावरणीय अध्ययन के ही अन्तर्गत छात्र को पृथ्वी, आकाश (अन्तरिक्ष), मौसम, मिट्टी एवं उपजों से इसका सम्बन्ध, बल, कार्य एवं ऊर्जा सामग्री तथा उनकी विशेषतायें, आवास एवं वस्त्र, जैविक वस्तुयें, मानव शरीर, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य आदि की विषय-वस्तु का अध्ययन कराया जाता है। इस तरह तीन से पाँच तक के छात्र पर्यावरणीय शिक्षा का अध्ययन करते हैं।
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय पाठ्यक्रम
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय पाठ्यक्रम निम्नानुसार हैं-
कक्षा 3 का स्तर - कक्षा 3 के स्तर तक निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है-
1. सजीवों का भोजन एवं पौधे- इसके अन्तर्गत जंगली जानवर तथा नदी, तालाब, समुद्र के जीव-जन्तु आदि आते हैं।
2. पानी के रूप का बदलना - इसके अन्तर्गत बर्फ, अँगीठी, स्टोव, हीटर आदि आते हैं।
3. पक्षियों के लक्षण - इसके अन्तर्गत पक्षियों के लक्षण जैसे- चोंच, पैर के विभिन्न रंग-रूप, पंखों का आकार, गाँव, कस्बे एवं जंगल आदि ।
4. मिट्टी में पानी रोक सकने की क्षमता - इसके अन्तर्गत लैम्प की चिमनी तथा गिलास आदि आते हैं।
5. विभिन्न प्रकार के पौधे - विभिन्न प्रकार के पौधों में मटर, सरसों, चना, हल्दी, शकरकन्द, आलू तथा अरबी आदि आते हैं।
6. पत्ती एवं पुष्प - विभिन्न प्रकार के पौधे जैसे लौकी, तरबूज, खरबूजा, अमरूद, खीरा, तौरई आदि ।
7. ईंधन - ईंधन के अन्तर्गत लकड़ी, मिट्टी का तेल, कोयला, गोबर के उपले एवं गैस सिलेण्डर आदि आते हैं।
8. ऊष्मा संचरण - इसमें गिलास, मोम, लोहे की छड़, स्याही आदि आते हैं।
कक्षा 4 का स्तर - कक्षा 4 के स्तर तक निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है-
1. ब्राह्माण्ड – इसमें आकाश, मोमबत्ती, उलकायें एवं गत्ते के डिब्बे आदि।
2. आकाश - इसके अन्तर्गत सूर्य, ग्लोबे, बल्ब एवं मोमबत्ती आदि ।
3. पृथ्वी - इसमें गेंद लट्टू एवं धागे के साथ लगा पत्थर आदि आते हैं।
4. जन्तु एवं वनस्पति - इसमें विभिन्न जन्तु एवं पक्षी तथा विभिन्न पौधे, मरुस्थलीय, जलीय एवं अन्य पौधे आदि आते हैं।
5. मिट्टी एवं चट्टान - इसके अन्तर्गत पर्वत, जंगल एवं पर्यावरणीय स्थल आदि आते
6. तापीय प्रसार - इसमें रेलवे लाइन, तार, टेलीफोन लाइन, गुब्बारा, शीशी एवं टब आदि आते हैं।
7. प्रकाश स्त्रोत - इसमें लालटेन, मोमबत्ती, बल्ब एवं सूर्य आदि आते हैं।
8. प्रकाश - इसमें सरल रेखागमन, बैटरी, मोमबत्ती, बल्ब तथा सूर्य आदि आते हैं।
कक्षा 5 का स्तर - कक्षा 5 के स्तर तक निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है-
1. जन्तु एवं वनस्पति जगत - इसके अन्तर्गत मछली, मेढ़क, विभिन्न पक्षियों की चोंच एवं पंजे, केकड़ा, कीड़े, मधुमक्खी, कॉकरोच, छिपकली तथा वनस्पतियों में चना, सरसों एवं मटर आदि आते हैं।
2. वायु दाब - इसमें गुब्बारा, ट्यूब, पिचकारी, गिलास, पैन, गत्ता, जल पम्प आदि आते हैं।
3. जल दाब एवं वायु - इसके अन्तर्गत स्टैण्ड, पंख एवं तीर, फिरकी, कटोरी एवं स्टैण्ड, बड़े आकार का डिब्बा, यू आकार की नली, जार तथा गुब्बारा आदि आते हैं।
4. हमारा शरीर - इसके अन्तर्गत माँसपेशियाँ, हड्डियाँ तथा सन्धियाँ आदि आते हैं।
5. सन्तुलित भोजन - सन्तुलित भोजन के अन्तर्गत प्रतिदिन आहार में प्रयोग होने वाली वस्तुयें घी, दूध, अण्डा, मक्का, ग्लूकोज, आलू, विभिन्न प्रकार के फल, पालक, मछली, माँस, अण्डे, मक्का, मूँगफली, मटर तथा गाजर आदि आते हैं।
6. कोशिका रचना - इसमें प्याज की झिल्ली, अमीबा तथा जन्तु कोशिका आदि।
7. ऊर्जा एवं कार्य - ऊर्जा तथा कार्य के अन्तर्गत डिब्बा, स्कूटर, चरखी, कार, मोमबत्ती, गिलास, स्याही, स्टोव, गेंद, पत्थर, अँगीठी आदि आते हैं।
8. पदार्थ की अवस्थायें - ठोस, द्रव एवं गैस आदि।
9. विद्युत ऊर्जा - बैटरी के सेल, बल्व, कील, लोहे का बुरादा आदि।
10. द्रव्यमान का घनत्व - नली सहित डिब्बा।
इन उपरोक्त सामग्रियों के अतिरिक्त अन्य सामग्री भी शिक्षक बनाकर पर्यावरण की शिक्षा को जीवन से सम्बद्ध कर सकते हैं।
राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नई दिल्ली द्वारा सन् 1975 में प्रकाशित दस वर्षीय स्कूल पाठ्यक्रम में विज्ञान की महत्ता इस प्रकार प्रतिपादित की है कि स्कूली छात्रों की सामान्य शिक्षा योजना में विज्ञान को स्थान दिये जाने का औचित्य आज निर्विवाद रूप से सिद्ध हो चुका है, क्योंकि विज्ञान सर्वव्यापी है। आधुनिक समाजों का अस्तित्व विज्ञान के आधार पर टिका है, क्योंकि विज्ञान का उत्पादन एवं संचार साधनों में घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसलिये वर्तमान स्थिति में जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को विज्ञान एवं तकनीकी की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्राथमिक कक्षाओं में विज्ञान पर्यावरण अध्ययन के रूप में अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाना चाहिये।
भारत की नई शिक्षा नीति, 1986 में भी विज्ञान के महत्व को स्वीकार कर स्कूली पाठ्यक्रम में विज्ञान शिक्षण के द्वारा छात्रों में वैज्ञानिक अभिवृत्ति एवं भौतिक, सामाजिक, तकनीक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पर्यावरण गति पर बल दिया है। इसीलिए नवीन राष्ट्रीय स्कूली पाठ्यक्रम, 1986 में प्राथमिक कक्षाओं के लिए सामान्य विज्ञान को पर्यावरण अध्ययन के रूप में एक अनिवार्य विषय का स्थान दिया तथा उसके लिये प्रति सप्ताह कालांशों में भी वृद्धि की है।
माध्यमिक स्तर पर पर्यावरणीय पाठ्यक्रम
माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में निम्न को सम्मिलित किया गया है-
1. अपने तथा दूसरे देशों में निश्चित अनुपात में संसाधनों का प्रयोग तथा इसके सम्बन्ध में अस्थिरता का अध्ययन।
2. प्राकृतिक संसाधनों का विभिन्न विभागों में जनसंख्या की डिग्री ऑफ एसेज के रूप में प्रयोग।
3. वैयक्तिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिस्थितिक एवं आर्थिक विकास की योजनायें।
विभिन्न श्रेणी के लोगों के लिए पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम के स्वरूप या विस्तार विभिन्न श्रेणियों के लोगों के लिये पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम को निम्नलिखित भागों में बाँटा जा सकता है-
1. औपचारिक पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम - इस श्रेणी में देश का सबसे बड़ा समूह विद्यार्थी जगत आता है, जो प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, सैकेण्डरी स्तर पर तथा विश्वविद्यालय स्तर पर विद्या अध्ययन करता है। आज का छात्र कल देश का कर्णधार तथा विश्व की ऊँचाई पर कहीं अधिक पहचान बनाने वाले व्यक्ति के रूप में उभरेंगे। इसलिये इनको पर्यावरण का ज्ञान कराना अत्यन्त आवश्यक है। अतः स्वयं अपने जीवन को सँवारे तथा अपने परिवार का मार्गदर्शन करें, समाज को नवीन दिशा दे तथा देश को पर्यावरण की समस्याओं से बचायें और अन्तर्राष्ट्रीय प्रयासों में सहयोग करें।
2. अर्द्ध-औपचारिक पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम - राष्ट्रीय योजनाओं एवं इसी प्रकार के अनेक कार्यक्रमों को बनाने के लिये तथा क्रियान्वयन करने एवं आवश्यकता पड़ने पर उनके परिणामों से सामना करने तथा उसका हल निकालने में प्रशासक, उच्च अधिकारी एवं निर्माणकर्त्ताओं की प्रमुख भूमिका रहती है। इसलिये इन सभी लोगों को पर्यावरण से सम्बन्धित जानकारी देनी चाहिये। सभी संस्थानों के अधिकारी एवं कर्मचारियों को भी पर्यावरण शिक्षा के कार्यक्रमों में भाग लेने के लिये आवश्यक कर दी जाये। यही नहीं बल्कि कारखाने, अस्पताल, इंजीनियरिंग संस्थान आदि के लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिये।
3. अनौपचारिक पर्यावरण शिक्षा पाठ्यक्रम - अशिक्षित और ऐसे लोग जो गाँवों में रहते हैं तथा जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से शिक्षा से कोई सम्बन्ध नहीं है, उनके लिये उनकी आवश्यकता के अनुसार ज्ञान एवं जानकारी उपलब्ध करानी चाहिये। पशु सुरक्षा, भूमि रख-रखाव, फसलों की कीड़ों से रक्षा, स्वच्छ आवास, स्वास्थ्य शिक्षा, रोग एवं उनसे बचने के उपाय, सिगरेट, तम्बाकू के सेवन से हानियाँ, मद्यपान निषेध आदि अनेक ऐसे ज्ञान के प्रकरण हो सकते हैं जो पर्यावरण के ही घटक हैं। इसके ज्ञान के लिये दूरदर्शन बहुत उपयोगी हो सकता है। इसके अलावा लघु नाटक, कठपुतली नाटक, गीत, लोकगीत, गाँवों के मेलों में प्रदर्शनियाँ आदि का आयोजन करना चाहिये।
इस प्रकार स्पष्ट होता है कि एक अच्छा सूचना संग्रहीत सन्तुलित सबकी रुचि का तथा पर्यावरणीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकने वाला पाठ्यक्रम निश्चय ही पर्यावरण शिक्षा को एक सफल कार्यक्रम के रूप में संचालित कर सकता है। अतः पाठ्यक्रम को इस शिक्षण प्रक्रिया में सर्वाधिक महत्त्व दिया जाना चाहिये।
|
|||||

 i
i