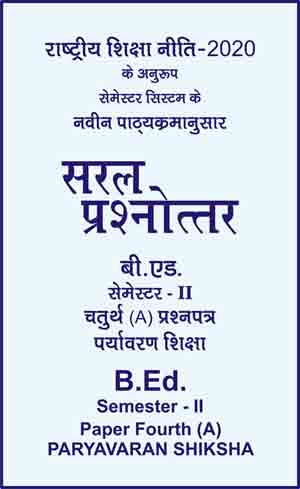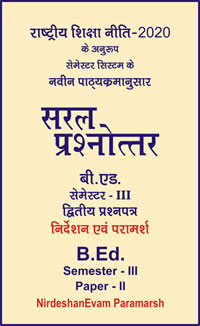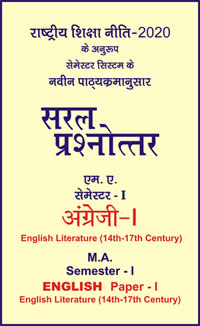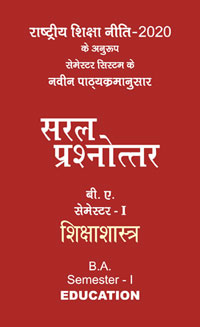|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षा बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा के स्वरूप की विवेचना कीजिए ।
उत्तर-
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा
प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य देश के पाँच से लेकर चौदह वर्ष तक के बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरुकता पैदा करना है। बच्चे किसी भी देश का भविष्य होते हैं। यदि बच्चों में अच्छी आदतों एवं विचारों को प्रारम्भ से ही समझाकर बताया जाये तो निश्चित ही उस देश का भविष्य उज्जवल होगा। कम आयु के बच्चों का मस्तिष्क बहुत अधिक कोमल एवं अविकसित होता है। अतः उन पर शिक्षा का अत्यन्त गहरा प्रभाव पड़ता है तथा वह लम्बे समय तक स्थायी बना रहता है। यदि छोटे बच्चों को पर्यावरण के विभिन्न पहलुओं से परिचित कराया जाये, तो वे आने वाले समय में इसे अच्छा बना सकेंगे। अतः हम इन्हें भविष्य का विशाल आधार कह सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा के द्वारा हम इस आधार को मजबूती प्रदान कर सकते हैं जिससे बड़े होकर आज के बच्चे एक स्वच्छ और अच्छे वातावरण में रह सकें।
नगरीय बालकों के लिये पर्यावरण शिक्षा की रूपरेखा- नगरीय बालकों में पर्यावरण के सम्बन्ध में निम्नलिखित पहलुओं के विषय में ज्ञान कराना तथा उन पर आचरण कराना विद्यालयी शिक्षकों का परम कर्तव्य है। पर्यावरण शिक्षा बालकों के पाठ्यक्रम का एक प्रमुख अंग होना चाहिये, क्योंकि इससे बालक पर्यावरण को समझने का प्रयत्न कर सकेंगे। ये पहलु निम्नलिखित हैं-
1. जल का उचित उपयोग - बालक जल के प्रयोग के प्रति अभी जागरूक नहीं है, क्योंकि वे बिना उपयोग के भी पानी उपयोग में लाते हैं। इसलिए नहाने धोने एवं कपड़े आदि धोने से नगर का पानी निरन्तर समय तक बहता रहता है। जल का संरक्षण करना बहुत अधिक आवश्यक है। अतः बालकों को जल के महत्व के बारे में जानकारी देना आवश्यक है। इसके लिये जल का उचित प्रयोग करने की शिक्षा प्रदान करना केवल शिक्षकों का ही कार्य नहीं है बल्कि माता-पिता तथा दूसरे समझदार लोगों का भी ये कर्तव्य है कि वे बालकों को जल का महत्त्व बतायें एवं समझायें और जल को व्यर्थ बहाने से उन्हें रोकें।
2. धूम्रपान का उपयोग न करें - आज छोटी-सी आयु में ही बालकों को धूम्रपान करने की आदत पड़ जाती है। धूम्रपान करने से खांसी, हृदय एवं फेफड़ों के रोग, पेट से सम्बन्धित विकार तथा कैंसर जैसे खतरनाक रोगों का जन्म होता है। बालकों को उन व्यक्तियों के पास जाने से भी रोकना चाहिये, जो धूम्रपान करते हैं। ऐसा करने से वे अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकेंगे।
3. कूड़े को चारों ओर न फैलायें - बालक कागज के टुकड़े, फलों के छिलके तथा अन्य कूड़ा इधर-उधर फेंकते रहते हैं। इस कूड़े से भूमि प्रदूषण बढ़ता है। अतः बालकों को यह बताना एवं समझाना बहुत आवश्यक है कि कूड़े तथा अन्य गंदगी को इधर-उधर न फेंककर कूड़े को केवल कूड़ेदान में ही डालें ।
4. खुले में शौच करना पर्यावरण के लिए हानिकारक - अधिकांश बच्चों को खुले में पेशाब एवं शौच करने की आदत होती है। ऐसा करने से भूमि प्रदूषित होती है। अतः पर्यावरण शिक्षकों का यह कर्त्तव्य है कि वे रोग फैलाने वाली गंदगी के प्रति बच्चों को सावधान करें।
5. जलती बत्ती को न छोड़ें - सामान्यतः बालक बिजली के उपयोग के प्रति लापरवाह होते हैं। यदि किसी कमरे में बत्ती जल रही है तो उसे बिना प्रयोग के ही जलता छोड़ दिया जाता है। इससे विद्युत का अनावश्यक अपव्यय होता है। इसकी पूर्ति करने के लिये विद्युत का अत्यधिक मात्रा में उत्पादन करना पड़ता है।
6. बच्चों को शराब की बुराई के प्रति जागरूक बनाना - शराब पीना स्वास्थ्य के लिये अत्यन्त हानिकारक है। शराब पीने से मानसिक विकास एवं हृदय रोग हो जाते हैं। इसे पीने से यकृत (लीवर) खराब हो जाते हैं। शराब पीकर वाहन चलाने से आये दिन अनेक दुर्घटनायें होती रहती हैं। अतः शराब न पीने के लिये बच्चों को जागरूक बनाना चाहिये ।
7. बच्चों को आस-पास के वातावरण का ज्ञान कराया जाये - पर्यावरण शिक्षकों का यह भी कर्तव्य है कि वे बच्चों को उनके आस-पास का ज्ञान करायें जिससे वे अपने पर्यावरण को अच्छी तरह समझ सकें। उन्हें समूहों में ले जाकर आसपास के कारखाने, तालाब, नदियाँ, उद्यान आदि को दिखाकर उनके विषय में तथा प्रदूषण के विषय में शिक्षा प्रदान की जानी चाहिये ।
8. बच्चों को जंगलों एवं वन्य जीवों के महत्त्व का ज्ञान कराया जाये - जंगलों एवं अन्य वन्य जीवों का पर्यावरण संतुलन में एक विशेष महत्त्व है। उन्हें इसका सम्पूर्ण ज्ञान कराना पर्यावरण शिक्षक का प्रथम कर्त्तव्य होना चाहिये।
9. बच्चों को जल एवं वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों के विषय में जानकारी दी जानी चाहिये - जीवों पर जल एवं वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभावों को कुछ प्रयोगों के द्वारा बच्चों को दिखाया जाना चाहिये। शिक्षकों को ऐसे प्रयोग विकसित करने चाहिये जिनसे प्रदूषण प्रभावों का जीता-जागता दृश्य उनके सामने प्रस्तुत किया जा सके।
10. बच्चों को पौधे लगाने के प्रति जागरूक किया जाये - पर्यावरण के लिये वृक्ष सबसे बड़े सहयोगी हैं। इनसे हमें ऑक्सीजन तो मिलती ही है, इसके साथ ही अनेकों औषधियाँ, ईंधन, एल्कोहल, रंग, भोज्य पदार्थ, फल, सब्जियाँ, आदि अनेक वस्तुयें प्राप्त होती हैं, लेकिन आज का मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिये निरंतर पेड़ों को काटता जा रहा है । इस क्षति की पूर्ति के लिये बच्चों को पौधे लगाने के लिए प्रेरित करना बहुत आवश्यक है। इसके अतिरिक्त यह भी बताना आवश्यक है कि वे अपने घरों में तथा गमलों में छोटे-छोटे पौधे लगायें क्योंकि पर्यावरण संतुलन के लिए वृक्षारोपण बहुत आवश्यक है।
ग्रामीण बच्चों के लिये पर्यावरण शिक्षा - ग्रामीण पर्यावरण की समस्यायें नगरीय समस्याओं से कुछ भिन्न भिन्न है। इसलिए कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें शिक्षा में सम्मिलित किया जा सकता है, लेकिन निम्नलिखित बातें ग्रामीण बच्चों के लिए बहुत अधिक आवश्यक है-
1. ग्रामीण बच्चे नहाने के लिए तालाब या पोखरों का उपयोग करते हैं। उन्हें इससे रोकना चाहिये एवं उन्हें यह बताना चाहिये कि प्रदूषित ( गंदे ) पाने में नहाने से अनेक विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं।
2. गाँवों के बच्चे व्यक्तिगत सफाई के प्रति लापरवाह होते हैं, इसलिए उन्हें व्यक्तिगत सफाई के महत्त्व के विषय समझाया जाना चाहिये।
3. ग्रामीण बच्चों को स्कूल एवं आस-पड़ौस की सफाई के विषय में विशेष शिक्षा प्रदान करनी चाहिये।
4. बच्चों को खेतों पर ले जाकर उन्हें कृषि एवं कृषि से सम्बन्धित फसलों की जानकारी एवं उनका ज्ञान कराना चाहिये।
5. ग्रामीण बच्चे खेतों या खुले में शौच करते हैं । अतः उन्हें यह बताना आवश्यक है कि शौच के बाद उसे मिट्टी से ढँक देना चाहिये ।
6. मक्खियों से भोज्य पदार्थों को बचाकर रखने एवं उससे होने वाले रोगों का ज्ञान कराया जाना चाहिये।
7. ग्रामीण बच्चों को यह सिखाया जाना आवश्यक है कि वे प्रत्येक समय नंगे पैर न घूमें फिरें, क्योंकि इससे अनेक रोगों के हो जाने का खतरा बना रहता है।
8. ग्रामीण बच्चों को जल एवं भोज्य पदार्थों को ढँककर रखने के लिए प्रेरित करना चाहिये।
इस प्रकार ग्रामीण एवं नगरीय बच्चों को समुचित पर्यावरण शिक्षा के ज्ञान एवं जानकारी के द्वारा एक ऐसा सुयोग्य नागरिक बनाया जा सकता है जो भविष्य में बिगड़ते हुए पर्यावरण की देखभाल करने में समर्थ हो सके।
|
|||||

 i
i