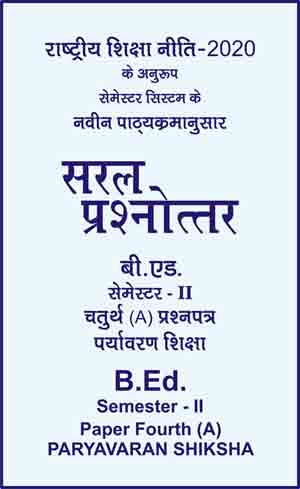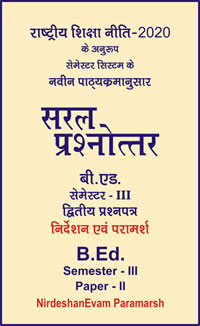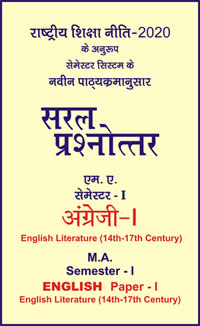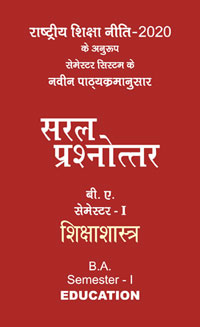|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षा बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- मीडिया या माध्यम से आप क्या समझते हैं? मीडिया का पर्यावरणीय शिक्षा में उपयोग बताइए।
उत्तर-
अंग्रेजी भाषा के शब्द 'Media' का अर्थ होता है - जनसंचार के साधन। हिन्दी भाषा में इसके लिए संचार शब्द का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार अंग्रेजी भाषा के शब्द 'Mass Communication" के लिए हिन्दी में जिस 'जन संचार' शब्द का प्रयोग होता है उसका अर्थ है- जनता या सामूहिक लोगों को सूचना आदि प्रदान करना। चूँकि अंग्रेजी भाषा में मास शब्द के अर्थ में मीन्स अर्थात् साधन शब्द का भी प्रयोग हुआ है। अतः मीडिया शब्द का अर्थ है - वे साधन, जिनके माध्यम से जनता या सामूहिक लोगों को सूचना प्रदान की जाती है।
अंग्रेजी भाषा के 'मॉस मीडिया' शब्द का सही रूपान्तर होगा- जनसंचार माध्यम या सामूहिकं माध्यम । जब किसी सूचना, समाचार, विचार आदि को दूर-दूर रहने वाले सभी व्यक्तियों तक पहुँचाने के लिए जिस माध्यम का प्रयोग किया जाता है, उसे जनसंचार माध्यम कहा जाता है।
जन-संचार माध्यम एवं सूचना-प्रौद्योगिकी - अनेकानेक सूचना-संसाधनों के प्रचलन से विश्व एक 'गाँव' के रूप में सिमट रहा है। इसके कारण प्रत्येक क्षेत्र में संक्रमण हुआ है। नई सूचना-तकनीकी ने मानव के समय और परिश्रम को बिल्कुल कम कर दिया है। आजकल मीडिया पर सूचना प्रौद्योगिकी का वर्चस्व स्पष्ट परिलक्षित हो रहा है। इसे निम्न शीर्षकों के अन्तर्गत सुविधाजनक ढंग से समझा सकता है-
(क) प्रिंट मीडिया
(ख) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया
(क) प्रिंट मीडिया - समाचार संकलन जनसंचार माध्यमों की कार्य- श्रृंखला का पहला कदम होता है। वर्तमान समय में समाचार संकलन हेतु मोबाइल फोन से लेकर लैपटॉप तक जैसे तकनीकी साधनों का प्रयोग किया जा रहा है। आज प्रिंट मीडिया पूरी तरह से तकनीकी साधनों व उपकरणों से सज्जित है। समाचार संकलन से लेकर छपाई तक का समस्त कार्य तकनीकी सुविधाओं से अत्यन्त कम समय में पूर्ण गुणवत्ता के साथ हो रहा है।
समाचार-पत्र का पूरा कार्यालय और उसका सम्पूर्ण कार्य कम्प्यूटर पर आधारित है। संवाददाता, ब्यूरोचीफ, समाचार सम्पादक आदि अपने-अपने डेस्क पर लगे कम्प्यूटर सेट पर समाचार को भाषायी, तकनीकी तथा संस्थान की नीति के आधार पर अन्तिम रूप देते हैं। सम्पादकीय विभाग, प्रोसेस यूनिट, विज्ञापन के बीच तालमेल बैठाने एवं फोटोग्राफी के सन्दर्भ में सूचना प्रौद्योगिकी की प्रभावकारी भूमिका है।
कुछ दिन पहले समाचार इकट्ठा करने के लिए संवाददाता इधर-उधर दौड़ते थे। गाँव-गाँव, तहसील तथा कस्बों से डाक द्वारा समाचार भेजे जाते थे। सम्पादकीय विभाग एक पोस्ट ऑफिस बना रहता था जहाँ पत्रों की छंटनी होती थी। समाचार संकलन के बाद सम्पादक समूह कलम घिसकर समाचार तैयार करता था। आज के तकनीकी युग में संचार के त्वरित साधनों, मुद्रण, सम्पादन, साज-सज्जा ने एक अप्रत्याशित रोमांचक यात्रा पूरी कर ली है। आज का पत्रकार मोबाइल, फैक्स, लैपटॉप, पेजर, इंटरनेट, ई-मेल से जुड़ चुका है। वह चाहे विश्व के किसी भी कोने में क्यों न हो, कुछ क्षणों में ही वहाँ के समाचार अपने कार्यालय या सम्पादक तक प्रेषित कर देता है। विशेषकर दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले समाचारों में देश-विदेश में नियुक्त प्रतिनिधि इस प्रौद्योगिकी के बल पर ही वहाँ की घटनाओं व घटना स्थलों के दृश्य हमारे सामने उपस्थित कर देतें हैं।
(क) इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - डा. अर्जुन तिवारी के शब्दों में- “प्रिंट मीडिया के साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी आई. टी. (इन्फोर्मेशन टेक्नोलॉजी अर्थात् सूचना प्रौद्योगिकी) से उपकृत है। समाचार संकलन से लेकर समाचार प्रसारण तक के विविध सोपानों की सफलता आई. टी. पर आश्रित है। न्यूज वेबसाइट और पोर्टल भी आई. टी. पर निर्भर है। वर्तमान मीडिया की पूरी कार्यप्रणाली में आई.टी. की भूमिका मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी जैसी हो गई है।"
आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का बड़ा स्पष्ट प्रभाव टी.वी. तथा फिल्मों में देखा जा सकता है। कैमरा ही इन दोनों माध्यमों का आधार है। कैमरा की गुणवत्ता में नई तकनीक के द्वारा क्रान्ति आई है । दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले समाचारों में इतना व्यापक परिवर्तन आया है कि देखने वाला आश्चर्यचकित रह जाता है। विश्व के किसी भी कोने में घटना घटित होने की देर नहीं होती कि वहाँ की वीडियो - ओडियो क्लिपिंग तुरन्त समाचारों में स्थान पा जाती है। वीडियो कान्फ्रेसिंग के द्वारा कहीं पर भी बैठकर व्यक्ति स्टूडियो के सम्पर्क में आ जाता है। ऑनलाइन तकनीक के द्वारा टी.वी. कार्यक्रम देखते समय वह अपने विचारों को भी कार्यक्रम के अन्तर्गत शामिल कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मल्टीमीडिया की भूमिका भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होती जा रही है।
मल्टीमीडिया से टी.वी. कार्यक्रमों में नई क्रान्ति आई है। इस तकनीक के द्वारा आज टी.वी. में निम्न सुविधाएँ देखने को मिलती हैं-
(1) टैक्स्ट - घटना या किसी वस्तु के बारे में सूचना जैसे- नोट्स, कान्टेन्ट्स।
(2) डाटा - टेबल, चार्ट, ग्राफ, स्टेटिस्टिक्स
(3) एनीमेशन - कम्प्यूटर द्वारा बनाये वीडियो।
(4) ऑडियो - स्पीच, संगीत जैसे-कैसेट्स, टेप, सी. डी.।
(5) वीडियो -फिल्म।
सूचना प्रौद्योगिकी के प्राप्त नए महत्त्व को देखते हुए भारत सरकार ने 15 अक्टूबर, 1999 में एक नये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का गठन किया। इस मंत्रालय का उद्देश्य भारत को सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विश्व के अन्य अग्रणी देशों की गिनती में शामिल करना है। सरकार इसी लक्ष्य को लेकर सॉफ्टवेयर निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ हार्डवेयर निर्माण और निर्यात को बढ़ाने का भी प्रयास कर रही है।
आज इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों में जिन सूचना तकनीकों का प्रयोग किया जा रहा है, वे निम्नलिखित हैं-
1. मल्टीमीडिया,
2. कंवर्जेंस,
3. कृत्रिम उपग्रह,
4. कम्प्यूटर,
5. इंटरनेट,
6. इंटरनेट
1. मल्टीमीडिया - मल्टीमीडिया टैक्स्ट, डाटा, चित्र, ऐनीमेशन, ओडियो एवं वीडियो का समन्वय है जिससे विभिन्न रूपों को एक डिजिटल माध्यम में बदलना और फिर उसे कम्प्यूटर द्वारा प्रेषण संभव होता है।.
मल्टीमीडिया का जन-संचार के क्षेत्र में कई उपयोग हैं, यथा-
(i) मल्टीमीडिया के द्वारा ई-मेल, वीडियोफोन, वीडियो, कॉन्फ्रेसिंग आदि।
(ii) पुस्तकालयों, संग्रहालयों, अस्पतालों एवं मान्यूमेण्ट्स आदि के सन्दर्भ में।
(iii) मनोरंजन सम्बन्धी सुविधा।
(iv) मल्टीमीडिया सूचना बैंक।
(v) मल्टीमीडिया सूचना संसाधन।
(vi) रिफरेन्स टूल्स जैसे- इनसाइक्लोपीडिया, शब्द-कोश।
(vii) प्रदर्शनियों में कान्फ्रेंस एवं ट्रेड शो।
(viii) उत्पादन सूचना कैटलॉग।
(ix) इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग।
(x) तकनीकी डाक्यूमेन्टेशन जैसे- अभियान्त्रिकीयं ड्राइंग, स्पेसीफिकेशन।
(xi) पर्यटन उपयोग हेतु सूचना सिस्टम डिजाइन।
मल्डीमीडिया ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा पाठ्य-पुस्तक, रंग, चित्र, फोटो, आवाज, जीव- संचारण और वीडियो के मिश्रण से कुछ नई रचना सामने आती है।
(2) कन्वर्जेन्स - आधुनिक विभिन्न तकनीकों का एक सम्मिश्रण कन्वर्जेन्स कहलाता है। आजकल इसका प्रचलन जनसंचार के नये रूप में किया जा रहा है। प्रसारण, केबल, कम्प्यूटरिंग, मल्टीमडिया, नेटवर्क, उपग्रह, दूर संचार का संगम ही अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी का वरदान है । इसने सारी दुनिया को एक समान धरातल पर खड़ा कर दिया
कन्वर्जेन्स टेलीकम्यूनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग तथा कम्प्यूटर नेटवर्किंग को सम्मिलित कर एक ऐसे एकल डिजिटल नेटवर्क का निर्माण करता है जिसके द्वारा टेलीफोन, टी. वी., फैक्स, इंटरनेट, वीडियोफोन, मूवी, संगीत, मनोरंजन आदि सुविधा एक ही माध्यम से प्राप्त हो जाती है।
(3) कृत्रिम उपग्रह - अन्तरिक्ष देवताओं का वास है, जैसी कल्पनाओं में प्राचीनकाल में मानव विचरण करता था। आधुनिक युग में मानव की पहुँच अन्तरिक्ष तक हो गयी है । अन्तरिक्ष तक पहुँच बनाये रखने के लिए उपग्रह निर्मित करना मनुष्य की एक महानतम उपलब्धि है। भारतीय अन्तरिक्ष कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य भारत के विकास के लिए अन्तरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग करना रहा है। इस दिशा में भारत ने विशेष प्रकार की अन्तरिक्ष प्रणाली की स्थापना की है अर्थात् आपदा चेतावनी प्रणाली के साथ दूरसंचार, दूरदर्शन प्रसारण तथा मौसम सम्बन्धी सेवाएँ देने के लिए भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली (इनसैट) तथा संसाधनों के प्रबन्ध के लिए भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह (आर.एस. एसव प्रणाली) । अतः कृत्रिम उपग्रह भी सूचना प्रौद्योगिकी का अहम हिस्सा है।
(4) कम्प्यूटर - आज कम्प्यूटर मानव का सबसे बड़ा मास्टर है। कम्प्यूटर अपनी असीम संग्रह क्षमता, तेजगति और आश्चर्यजनक परिणाम देने की क्षमता के कारण अपनी पृथक् पहचान बनाने में सफल हुआ है। आज हम उच्च तकनीकी, सुपर कम्प्यूटरों और इंटरनेट की दुनिया में हैं। रेडियो, टी.वी. तथा फिल्म जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आज पूरी तरह कम्प्यूटर के प्रभाव में हैं।
(5) इंटरनेट - सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण संचार साधन इंटरनेट इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शनों की एक विशाल प्रणाली है जो बिजली की भाँति आधुनिक जीवन का एक अंग है। आज घर पर बैठकर युवा वर्ग को (On Line Education) प्राप्त हो रही है। अब वह दिन दूर नहीं है जब इस नित बदलती तकनीक में रोबोट समाचार लिखते दिखेंगे।
आज से तीन दशक पहले 'गार्जियन' अखबार के कॉलम लेखक माइकल फ्रेन अपने उपन्यास में लिखा था - "वह दिन आएगा जब संवाददाता की जगह मशीन ले लेगी।" तब यह बात कपोल कल्पना ही प्रतीत हुई होगी पर आज यह शत-प्रतिशत सत्य दीख रही है ।
(6) इंटरनेट - वस्तुतः यह सुविधा किसी कम्पनी या संस्था का निजी कम्प्यूटर नेटवर्क होता है जो किसी सार्वजनिक नेटवर्क की तरह कार्य करता है, परन्तु यह कम्पनी के आन्तरिक प्रयोग तक सीमित रहता है। दृश्य-श्रव्य तथा श्रव्य जनसंचार माध्यमों में इस इंटरनेट प्रौद्योगिकी का भी विशेष महत्त्व है। कभी-कभी समाचार वाचक समाचार वाचन के दौरान ही प्राप्त किसी नवीन व महत्त्व पूर्ण समाचार के सन्दर्भ में 'अभी-अभी प्राप्त सूचना के अनुसार ......... कहकर उसे उद्घोषित करता है। उसे यह सूचना इंटरनेट के माध्यम से ही मिलती है। इसके अतिरिक्त कम्पनी या संस्था की विभिन्न शाखाओं के बीच सूचनाओं के तीव्रगामी आदान-प्रदान के लिए इंटरनेट उपयोगी सिद्ध हुआ है।
मीडिया का पर्यावरणीय शिक्षा में उपयोग
पर्यावरणीय शिक्षा में मीडिया का बहुत उपयोग है। मीडिया के द्वारा पर्यावरण जागरुकता अभियान चलाया जाता है। न्यूज पेपर, मैगजीन, रेडियो, टी.वी. आदि के द्वारा जन समूहों को पर्यावरण सम्बन्धी मुद्दों एवं समस्याओं के प्रति शिक्षित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। लोकगीतों, नुक्कड़ नाटकों, डॉक्यूमेंटरीज के द्वारा लोगों में पर्यावरणीय जागरुकता फैलाई जा सकती है। गाँवों एवं दूर-दूराज के इलाकों में विज्ञान केन्द्र स्थापित कर पर्यावरणीय समस्याएँ, उनके कारण एवं निवारक उपाय आदि को प्रभावी ढंग से लोगों के बीच में फैलाया जा सकता है। मीडिया में लोकप्रिय एवं प्रख्यात् लोगों को शामिल कर पर्यावरणीय मुद्दों के महत्त्व की समझ एवं प्रवर्तन को बढ़ाया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन एवं पर्यावरण की समझ के विकास हेतु आम जन के जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि उन्हें यह ज्ञात हो कि हमारे वातावरण में जो परिवर्तन हो रहे हैं उनके द्वारा मानव जीवन कैसे प्रभावित हो रहा है। इन सब की जानकारी आम जन को मीडिया के द्वारा दी जा सकती है।
|
|||||

 i
i