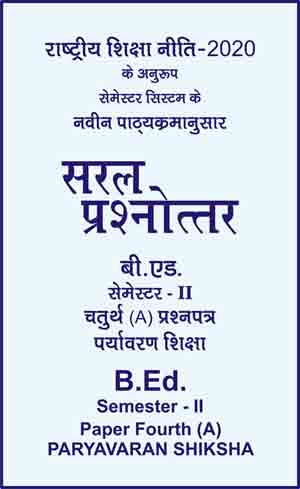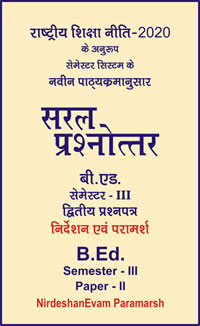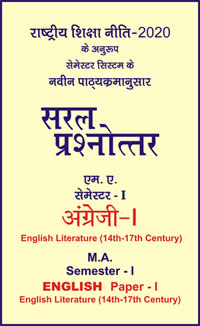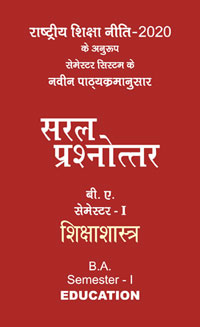|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षा बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? छात्रों के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का क्या महत्त्व है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं का संगठन कैसे किया जा सकता है? विवेचना कीजिए।
अथवा
पर्यावरणीय शिक्षा में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का वर्णन कीजिए।
उत्तर-
विद्यालयों में शिक्षण के साथ जो अन्य क्रियाएँ, यथा-खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रतियोगिताएँ आदि संचालित होती हैं, उनहें पाठ्य सहगामी क्रियाएँ कहते हैं। शिक्षाविदों ने उन्हें इस प्रकार व्यक्त किया है-
फ्रोबेल - "यदि हम सम्पूर्ण मानव को विकसित करना चाहते हैं, तो हमें उन्हें व्यायाम कराना चाहिए।"
विवेकानन्द - “आज भारत को भगवद्गीता की नहीं वरन् फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता है।"
इस प्रकार से उक्त शिक्षाविदों के कथन से स्पष्ट है कि खेल-कूद सम्बन्धित क्रियाएँ विभिन्न दृष्टि से महत्त्वपूर्ण होती हैं, किन्तु उसके गठन के समय अवश्य ही ध्यान देना चाहिए।
शिक्षा सर्वांगीण विकास की एक प्रक्रिया है, जिसका लक्ष्य वर्तमान समय में अतिव्यापक हो गया है। शिक्षा के लक्ष्य की व्यापकता ने पाठ्यक्रम को अति व्यापक बना दिया है। अब पाठ्यक्रम में शिक्षकों एवं छात्रों के बीच की समस्त अन्तर्क्रियाएँ उन्हें परस्पर सम्पर्क में लाती हैं, जो विद्यालय परिसर के अन्दर या बाहर घटित होती हैं। इस अर्थ में पाठ्यक्रम की सहगामी क्रियाएँ पाठ्यक्रम की अभिन्न अंग हैं।
1. स्वास्थ्य एवं मनोरंजन से सम्बन्धित क्रियाएँ - इन क्रियाओं को सहगामी क्रियाओं में विशेष महत्त्व दिया गया है। इनमें निम्नलिखित क्रियाएँ आती हैं-
(i) खेलकूद से सम्बन्धित क्रियाएँ - इसके अन्दर सभी प्रकार के खेलकूद आ जाते हैं। कम या अधिक मात्रा में सभी विद्यालयों में इनके लिए व्यवस्था है, जिस विद्यालय का आर्थिक स्तर जिस ढंग का होता है वहाँ उसी स्तर तक के खेलकूदों की व्यवस्था होती है ।
(ii) व्यायाम - खेलकूद के अलावा अच्छे विद्यालयों में एक व्यायामशाला होती है, जहाँ छात्रों को अनेक प्रकार के शारीरिक व्यायाम सिखाये जाते हैं।
(iii) विद्यालय के उत्सव - विद्यालयों में उत्सवों का आयोजन मनोरंजन की दृष्टि से किया जाता है इसके अन्तर्गत विद्यालय के वार्षिकोत्सव एवं राष्ट्रीय पर्व सम्मिलित किये जाते हैं।
2. सांस्कृतिक क्रियाएँ - बालकों के चारित्रिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास में सांस्कृतिक क्रियाओं का बड़ा महत्त्व होता है। इन सांस्कृतिक क्रियाओं के कुछ विषय निम्न हैं-
(i) नाटक
(ii) लोकगीत, संगीत, प्रहसन और कैम्फायर आदि का आयोजन।
3. साहित्यिक क्रियाएँ - विद्यालय में सहगामी क्रियाओं के रूप में साहित्यिक क्रियाओं का बड़ा महत्त्व है। इन साहित्यिक क्रियाओ से बालकों में साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न होती है और अध्ययन के लिए प्रेरणा मिलती है। साहित्यिक क्रियाओं में निम्नलिखित प्रमुख हैं-
(i) साहित्यिक प्रतियोगिताएँ - साहित्यिक प्रतियोगिताओं में नाटक, कहानी, निबन्ध, कविता आदि प्रतियोगिता के लिए लिखना पड़ता है। इन प्रतियोगिताओं में बालक द्वारा लिखी रचनाओं को ही लिया जाता है। विद्यालय में वाद-विवाद प्रतियोगिताओं को भी साहित्यिक प्रतियोगिताओं में स्थान दिया जाता है।
(ii) वार्षिक पत्रिकाएँ - विद्यालय के छात्रों एवं अध्यापकों के सहयोग से पत्रिकाएँ निकलती हैं, जिनमें उनका लेख प्रकाशित होता है।
(iii) भाषण - माला का आयोजन-अच्छे विद्यालयों में एक भाषण - माला का आयोजन होता है, जिसमें विद्यालयों के अध्यापक एवं बाहरी विद्वानों को भी आमन्त्रित किया जाता है।
कवि सम्मेलन एवं कवि दरबार भी साहित्यिक सहगामी क्रियाओं में सम्मिलित किये जाते हैं।
4. सामाजिक क्रियाएँ - आजकल शिक्षा में सामाजिक क्रियाओं का बोलबाला होता है। अनेकानेक उपायों द्वारा बालकों में सामाजिक विकास लाने का प्रयास किया जा रहा है। यद्यपि बालकों के सामाजिक विकास में सभी क्रियाओं का सहयोग होता है, पर निम्नलिखित क्रियाओं का उसमें विशेष महत्त्व होता है-
(i) श्रमदान - प्रत्येक विद्यालय में पाठ्यक्रम में श्रमदान को स्थान दिया गया है। उसमें पारस्परिक सहयोग से बालकों में सामाजिकता का बहुत अधिक विकास होता है।
(ii) युवक मंगल दल - वर्तमान समय में विद्यालय एवं समाज को एक-दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया जा रहा है। विद्यालय को समाज के निकट लाकर उनकी समस्याओं का अध्ययन करना चाहिए। अतएव विद्यालयों में ऐसी अनेक समितियाँ बनायी जाती हैं, जो गाँवों में जाकर गाँव के विकास में योगदान देती हैं।
(iii) छात्र समितियाँ - विद्यालयों के जनतन्त्रीय भावना की शिक्षा देने के लिए आवश्यक है कि छात्रों को जनहित के कार्यों में योग देने के लिए प्रोत्साहित किया जाये। इस सम्बन्ध में विद्यालय के कार्यों में भाग लेने के लिए छात्र सिमितियाँ बनायी जाती हैं। उपर्युक्त सहगामी क्रियाओं के अलावा स्काउटिंग, सैनिक शिक्षा, पिकनिक आदि अन्य सहगामी क्रियाएँ भी सम्मिलित की जाती हैं।
पाठ्य सहगामी क्रियाओं के संगठन के सिद्धान्त - विद्यालयों में पाठ्यक्रम की सहगामी क्रियाओं के संगठन एवं उनकी सफलता के लिए निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना चाहिए-
(i) विद्यालय में किसी क्रिया के संचालन के पूर्व छात्रों एवं अध्यापकों के सहयोग से एक योजना का निर्धारण आवश्यक है।
(ii) विद्यालय में उसी क्रिया का संगठन किया जाये, जो विद्यालय की उद्देश्यपूर्ति में सफल हो।
(iii) योजना निर्माण में प्रधानाचार्य के सुझावों का भी ध्यान रखना चाहिए।
(iv) यद्यपि इन क्रियाओं की सफलता छात्रों पर ही निर्भर करती है, परन्तु अध्यापकों का यथासमय निर्देशन अति आवश्यक है।
(v) अध्यापकों को सहगामी क्रियाओं के संरक्षण का उत्तरदायितव उनकी रुचि एवं योग्यता को ध्यान में रखते हुए देना चाहिए।
(vi) इन क्रियाओं का समान दायित्व प्रत्येक अध्यापक पर होना चाहिए।
(vii) इन क्रियाओं के सम्बन्ध में उचित निर्देशन की व्यवस्था विद्यालयों में होनी चाहिए।
(viii) इन क्रियाओं को प्रारम्भ करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इन्हें धीरे-धीरे प्रारम्भ करना चाहिए और विद्यालय की आर्थिक क्षमता के अनुसार आगे बढ़ाते रहना चाहिए।
(ix) प्रत्येक बालक को इन क्रियाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
(x) इन क्रियाओं की सदस्यता सबके लिए खुली होनी चाहिए।
(xi) क्रियाओं की तालिका बनाते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि पढ़ाई-लिखाई के कार्यों से इसमें बाधा न पड़ने पाये ओर खाली समय का अधिक से अधिक सदुपयोग हो सके।
इस प्रकार से तैयार किया गया पाठ्यक्रम बालकों की आयु, रुचि, योग्यता एवं ग्रहण करने की क्षमता पर आधारित होगा।
पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्त्व
बालकों के व्यक्तित्व के पूर्ण विकास में पाठ्य सहगामी क्रियाओं का विशेष योगदान है। सामाजिक गुणों का विकास बहुत कुछ सहगामी क्रियाओं पर निर्भर करता है। पाठ्य सहगामी क्रियाओं का महत्त्व निम्नलिखित है-
1. ये क्रियाएँ पाठ्यक्रम को रोचक बनाती हैं - सहगामी क्रियाएँ बालकों को अवकाश प्रदान करके उनकी मानसिक थकान दूर करती हैं। इसके अभाव में पाठ्यक्रम की दशा उस मार्ग जैसी हो जाती है, जिस पर मुसाफिरों के आराम, मनोरंजन एवं खाने-पीने की व्यवस्था नहीं रहती।
2. अवकाश के समय का सदुपयोग - निरन्तर पढ़ते रहने से बालक ऊबने लगते हैं । अतएव उन्हें अवकाश देना आवश्यक हो जाता है। सहगामी क्रियाओं से बालकों के समय का सदुपयोग हो जाता है।
3. स्वानुशासन - बच्चों को स्वानुशासित रहने का जितना अवसर सहगामी कियाओं से मिलता है, उतना कक्षा में कार्यों से नहीं। सच्चा अनुशासन बालकों में उनकी स्वतन्त्रता में देखने को मिलता है।
4. सामाजिक विकास - स्वतंत्र वातावरण में परस्पर एक-दूसरे के साथ हिल-मिलकर काम करने से सामाजिक गुणों का विकास होता है। सामाजिक गुणों के विकास का अवसर जितना स्वतंत्र वातावरण में मिलता है, उतना कक्षा में नहीं। बालक एक-दूसरे के सम्पर्क में तभी आते हैं, जब उनको साथ मिलकर काम करने का अवसर मिलता है।
5. शारीरिक विकास - विद्यालय का कार्य स्वस्थ्य नागरिकों का निर्माण करना है। स्पष्ट है कि शारीरिक विकास का अवसर सहगामी क्रियाओं से प्राप्त होता है।
6. मानसिक विकास - सहगामी क्रियाओं से बालकों में मानसिक विकास होता है। स्वतंत्र एवं पारस्परिक रूप से कार्य करने से उनका मस्तिष्क अधिक विकसित होता है। पारस्परिक सहयोग से बालकों में आत्मनियन्त्रण का विकास होता है। इसमें उनको सोचने समझने व तर्क करने का पर्याप्त अवसर मिलता है।
7. संवेगात्मक विकास - बालकों को अपनी मूल प्रवृत्तियों एवं संवेगों के परिष्कार एवं परिशोधन के लिए जितना अवसर सहगामी क्रियाओं से मिलता है उतना अन्यत्र नहीं। इससे बालकों में आत्माभिव्यक्ति के गुणों का विकास होता है।
8. चारित्रिक विकास - बालकों के चरित्र-निर्माण की शिक्षा सहगामी क्रियाओं के माध्यम से प्राप्त होती है।
9. मनोरंजन - मानव स्वभावतः मनोरंजन की आवश्यकता का अनुभव करता है। पाठ्यक्रम की सहगामी क्रियाएँ बालकों के मनोरंजन का सर्वोत्तम साधन हैं। इसमें बालक अपना मनोरंजन अपने आप कर लेते हैं।
10. विद्यालय का आर्थिक लाभ - सहगामी क्रियाओं में छात्र समितियाँ एवं श्रमदान भी आते हैं। इनके माध्यमों से विद्यालय में अधिकांशतः आर्थिक बचत हो जाया करती है।
11. विद्यालय और समाज के बीच समन्वय - विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, जिसका निर्माण विद्यालय अपनी हित के लिए करता है, इसलिए इन दोनों का सम्बन्ध जरूरी है। विद्यालय एवं समाज को एक-दूसरे के निकट लाने वाले साधनों में सहगामी क्रियाएँ प्रमुख हैं।
|
|||||

 i
i