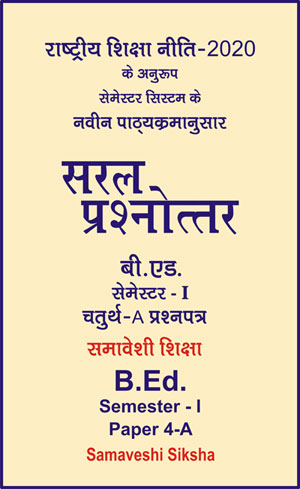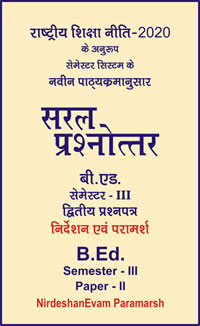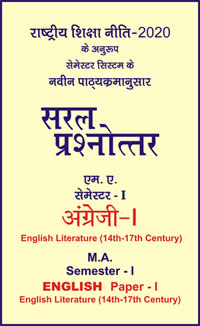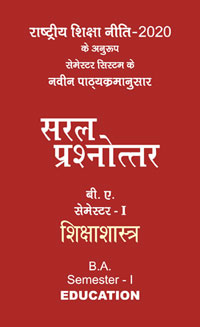|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- अवांछित वर्ग के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का विस्तृत वर्णन कीजिए।
अथवा
वंचित वर्ग के बालकों के प्रकार बताइए।
उत्तर -
समाज के वह वर्ग जो कथित रूप से छोटी जाति, क्षीण आर्थिक स्थिति (निर्धनता) होने के कारण उन्हें पढ़ने-लिखने तथा आगे बढ़ने के अवसरों से वंचित कर दिया गया है, कहीं-कहीं लिंग भी प्रभावी होता है। ऐसे बच्चों जिन्हें अवसरों की समानता प्राप्त नहीं है, अवांछित वर्ग के बच्चे कहलाते हैं।
वंचित बालकों के प्रकार -
- अनुसूचित जनजाति के बच्चे (ST)
- अनुसूचित जाति के बच्चे (SC)
- पिछड़े वर्ग के बच्चे (OBC)
- अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चे (Minority)
- बालिका वर्ग (Girls)
1. भारत में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जातियों के बच्चों की शिक्षा -
- भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 में "अनुसूचित जनजातियां" वे जातियां प्रायः पहाड़ी, पिछड़े जंगलों क्षेत्रों में रहती हैं, जिन्हें आदिवासी भी कहा जाता है। इसमें समय-समय पर मानकों के अनुसार परिवर्तन किया जाता है।
- अनुसूचित भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के प्रावधानों के तहत अनुसूचित वे जातियां हैं, जो समाज में विभिन्न कारणों से पिछड़ी हैं।
- राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में इनकी शिक्षा व्यवस्था हेतु अनेक घोषणाएं की गई हैं और घोषणाओं के साथ-साथ अनुसूचनाओं हेतु कुछ योजनाएं POAभी प्रस्तुत की गई हैं। इनमें मुख्य घोषणाएं -
- नगरों, गांवों और पहाड़ी तथा आदिवासी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के बच्चों के लिए विद्यालयों की स्थापना की गई है।
- इन विद्यालयों में यथासंभव इन्हीं वर्गों के और क्षेत्रों के शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी।
- दूर-दराज से आने वाले बच्चों के लिए छात्रावास की व्यवस्था की जाएगी।
- इन वर्गों के बच्चों को आर्थिक सहायता की धारा जारी बढ़ाई जाएगी।
- आदिवासी क्षेत्रों में पहले उनकी भाषा सिखाई जाएगी और उसके बाद क्षेत्रीय भाषा सिखाई जाएगी।
इन घोषणाओं के अनुसार वर्तमान में शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं -
- सर्व शिक्षा अभियान (S.S.A.) के अंतर्गत इनके क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालय, अंगनवाड़ी और नए प्रकार के शिक्षा केंद्र खोलने को प्राथमिकता दी जा रही है।
- सभी प्रांतों में इस वर्ग के बच्चों को प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर पर पाठ्यपुस्तकें, वस्त्र एवं मध्याह्न भोजन भी निःशुल्क प्रदान किए जाते हैं।
- इनके लिए छात्रावासों का निर्माण भी किया जा रहा है।
- इस समय केंद्र सरकार प्रांतीय सरकारों को अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जातियों की शिक्षा हेतु ब्लॉक अनुदान देती है जिससे प्रांतीय सरकारें विभिन्न शैक्षिक योजनाओं पर व्यय करती हैं।
- माध्यमिक एवं उच्च स्तर के छात्र-छात्राओं के लिए विशेष छात्रवृत्तियों की व्यवस्था की गई है।
- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (U.G.C.) भी इन वर्गों के छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु बड़ी संख्या में जूनियर और सीनियर फैलोशिप दे रहा है।
2. पिछड़े जाति वर्ग के बच्चों की शिक्षा -
भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के अनुसार सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़ी जातियां पिछड़े वर्ग में आती हैं। समय-समय पर आयोग समय पर आयोग का निर्माण किया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में इस वर्ग में आने वाले बच्चों की शिक्षा व्यवस्था हेतु अनेक कार्य योजनाएं संशोधित की गई हैं। इन घोषणाओं और कार्य योजनाओं के अनुसार वर्तमान में पिछड़े वर्ग एवं पिछड़े वर्ग की शिक्षा व्यवस्था हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं -
- सर्व शिक्षा अभियान (S.S.A.) के अंतर्गत इनके क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल खोलने को विशेष प्राथमिकता दी जा रही है।
- माध्यमिक एवं उच्च स्तर पर इनको आर्थिक सहायता दी जा रही है।
- इस वर्ग के बच्चों के लिए कुछ विशेष छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की गई है।
3. अल्पसंख्यक वर्ग के बालकों की शिक्षा -
भारत में धर्म और भाषा के आधार पर कुछ वर्गों के व्यक्तियों को अल्पसंख्यक घोषित कर दिया गया है। इनमें मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन, सिख आदि आते हैं। परंतु ईसाई, बौद्ध और जैन शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं। इसलिए जब शिक्षा के क्षेत्र में अल्पसंख्यकों की शिक्षा की चर्चा की जाती है तो विशेषकर मुसलमान बच्चों की शिक्षा की बात की जाती है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में अल्पसंख्यकों की शिक्षा के सम्बन्ध में दो प्रावधान किए गए हैं -
- धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि से शिक्षा संस्थाओं को स्थापना और प्रबंधन का अधिकार होगा।
- शिक्षा संस्थानों को सहायता देने में राज्य किसी विद्यालय के विरुद्ध इस आधार पर भेद नहीं करेगा कि वह धर्म या भाषा पर आधारित किसी अल्पसंख्यक वर्ग के प्रबंधन में है।
वर्तमान में अल्पसंख्यकों के बच्चों की शिक्षा हेतु निम्नलिखित प्रयास किये जा रहे हैं -
- सर्व शिक्षा अभियान (S.S.A.) के अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के साथ अल्पसंख्यकों के क्षेत्रों में भी प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्कूल स्थापित करने को प्राथमिकता दी जा रही है।
- शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यकों के लिए क्षेत्रीय सघन कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- मदरसा शिक्षा के आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता दी जा रही है।
- इनकी कुछ जातियों को पिछड़ी जातियों की सूची में स्थान दिया गया है और उनको यथा आश्रय व आर्थिक सुविधाएँ प्रदान की जा रही हैं।
4. बालिका-वर्ग की शिक्षा
भारत वर्ष के आजाद होने के बाद सर्वप्रथम राधाकृष्णन कमेटी (1948-49) ने स्त्री शिक्षा की सुव्यवस्थित व्यवस्था करने का सुझाव दिया। 1951 में बालिका शिक्षा के प्रचार तथा प्रोत्साहन के लिए योजनाओं पर कार्य शुरू किया गया। 1958 में केंद्र सरकार ने स्त्री शिक्षा के महत्व पर सुझाव देने के लिए श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख की अध्यक्षता में राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति का गठन किया। इस अध्यक्ष के नाम पर विशेष महिला शिक्षा संस्थानों की स्थापना, स्त्री शिक्षा का प्रचार-प्रसार हेतु विशेष सुझाव दिए, जिनमें राष्ट्रीय और स्त्री-पुरुषों हेतु शिक्षा का सुझाव मुख्य था। 1959 में राष्ट्रीय महिला परिषद का गठन हुआ तथा 1962 में स्त्री शिक्षा समिति का गठन किया गया।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में स्त्री शिक्षा के उन्नयन के लिए निम्नलिखित घोषणाओं को गई और कार्य योजनाएं भी प्रस्तुत की गईं:
- बालिका-बालकों की शिक्षा में भेद नहीं किया जाएगा।
- जिन जिलों में स्त्री साक्षरता प्रतिशत बहुत कम है, उनमें जिला विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
- बालिका निर्भरशिक्षा शिक्षा केंद्रों को 90 प्रतिशत अनुदान देना शुरू किया गया है।
- 1989 में महिला साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया जो वर्तमान में 900 ग्रामों में चलाया जा रहा है। इसके द्वारा ग्रामीण और पिछड़े वर्ग की बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था की जा रही है।
- सरकारी विद्यालयों में बालिकाओं के लिए 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गए हैं।
- माध्यमिक और उच्च प्राथमिक स्तर तक की शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है, कुछ प्रांतों में उच्च शिक्षा भी निःशुल्क है।
- गरीब वर्ग की छात्राओं को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है।
- उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए कुछ विशेष छात्रवृत्तियों की भी व्यवस्था की गई है।
मलिन बस्तियों के बच्चों की शिक्षा
विकासशील देशों में मलिन बस्तियाँ (Slum areas) नगरीय अनुसंधान एवं औद्योगीकरण का परिणाम है। मलिन बस्तियाँ शहरों में अवस्थित ऐसे क्षेत्र होते हैं, जिनमें निम्न स्तर की आवास व्यवस्था होती है। एक मलिन बस्ती सदैव एक ऐसा क्षेत्र होता है, जिसमें एक या अधिक आवास होते हैं। यहाँ निम्न आर्थिक स्तर पर उच्च अपराध दर पाई जाती है।
मलिन बस्तियों में रहने वाले प्राथमिक स्तर पर शिक्षा अभियानकर्ताओं के बीच प्रतिशत बच्चों निरक्षर हैं। ऐसे परिवारों में प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने वाले बच्चों की संख्या 30.58 प्रतिशत है। मलिन बस्तियों में निर्धनता व्याप्त है, जिसके कारण वे शिक्षा पर व्यय नहीं कर पाते हैं। साथ ही वहां शिक्षा का वातावरण नहीं होता है। सर्वप्रथम 1957 में मलिन बस्ती उन्नयन योजना शुरू की गई, जिसमें विद्यालय बनाए गए। इन बस्तियों में आवासीय समस्या का निदान आवश्यक प्राथमिकता है। मलिन बस्तियों में जागरूकता की अभाव है, जिसके कारण वे सरकार द्वारा दी गई सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाते हैं। बच्चे छात्रवृत्तियाँ एवं निःशुल्क पुस्तकें एवं अन्य सरकारी सुविधाओं का भी लाभ नहीं उठा पाते हैं।
|
|||||

 i
i