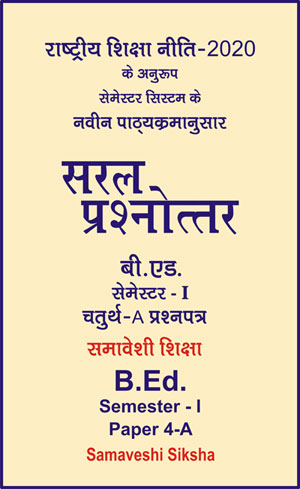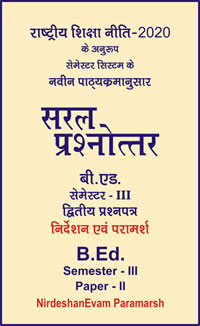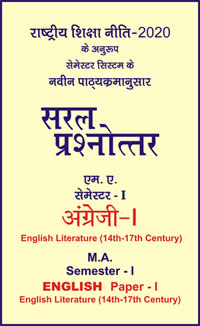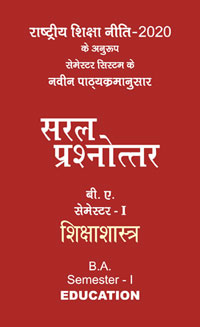|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- शारीरिक रूप से निशक्त, दुर्बल, क्षीण विकलांग बालक से आप क्या समझते हैं? इनकी शिक्षा हेतु आप क्या विशेष व्यवस्था करेंगे।
अथवा
निशक्त या विकलांग बालकों की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए?
अथवा
निशक्त या विकलांगों की शिक्षा के उद्देश्य लिखिए।
अथवा
निशक्त या विकलांग बालकों की शिक्षा में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए।
अथवा
शारीरिक बाधित बालक की समस्याएँ क्या हैं?
उत्तर -
निशक्त या विकलांग बालकों की समस्याएँ
बालक अपंग हों, अंधे हों, आधे अंधे हों, पूर्ण बहरे हों या अपूर्ण बहरे हों अथवा वे मानसिक रूप से अपंग या विकलांग हों, ऐसे बालकों को विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों की इन समस्याओं की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है।
शारीरिक दोषों के परिणामस्वरूप बालकों को हर क्षेत्र में समाजोपयोग संबंधी कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ऐसे अपंग बालकों में संवेगात्मक परिपक्वता नहीं आती। इन बालकों में हीन भावना उत्पन्न हो जाती है और वे अधिकतर क्रियाओं में भाग नहीं लेते। इन्हें अपनी इच्छाओं को दबाना पड़ता है, जिससे मन में यह बात घर कर जाती है कि अन्य लोग भी उन्हें तिरस्कार की दृष्टि से देखते हैं।
ये विचार के परिणामस्वरूप इनका संवेगात्मक संतुलन स्थिर नहीं होने के कारण वे स्वयं को अन्य बालकों में समायोजित नहीं कर पाते। विकलांगों या अपंगों के समायोजन से सम्बंधित समस्याओं पर शिक्षकों को सहानुभूतिपूर्ण विचार करना चाहिए।
कक्षा में शारीरिक रूप से अपंग बालकों को बैठने की समस्या का सामना करना पड़ता है। ऐसे बालकों को कक्षा में बिठाने के लिए विशेष प्रकार की कुर्सी-मेज़ की व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि कक्षा में कार्य करते समय उन्हें किसी प्रकार से कोई असुविधा न हो।
इसी प्रकार कक्षा में अन्य अंधे और अर्ध-अंधे बच्चों को भी बैठने की समस्या का सामना करना पड़ता है। उन्हें श्यामपट्ट से इतनी दूर बिठाया जाना चाहिए कि श्यामपट्ट पर लिखे शब्द उन्हें स्पष्ट दिखाई दें। पूर्ण या अपूर्ण बहरे बच्चे सुनने की समस्या का सामना करते हैं।
उन्हें सुनने की उचित सुविधा दी जानी चाहिए ताकि वे सामान्य बालकों के साथ संवाद कर सकें और उनके होठों की हलचल को अनुकृत करके कुछ सीख सकें। ऐसे बच्चे प्रायः उत्तेजक प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे बच्चों को विशेष प्रकार के व्यवहार की आवश्यकता होती है।
बोलने में कठिनाई - ऐसे बालकों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। शब्दों को बार-बार बुलवाना चाहिए। दोषपूर्ण वाणी वाले बच्चों को हीन भावना की समस्या का सामना करना पड़ता है। अतः ऐसे बालकों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।
मानसिक रूप से अपंग बालकों की समस्याएँ
मानसिक रूप से अपंग बालकों का समायोजन सम्बन्धी मुख्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे परिवार में समायोजन सम्बन्धी समस्या, स्कूल में समायोजन की समस्या, समाज में समायोजन की समस्या। मानसिक रूप से अपंग बालक स्वयं को घर, स्कूल और समाज में हीनभावना महसूस करता है। उसे अपनी असफलताओं से निराशा होने लगती है और वह कठिनाई महसूस करता है। दूसरे लोगों की निगाहों में वह निम्न स्तर का बनकर रह जाता है। स्कूल में अन्य विद्यार्थियों में वह रुचि नहीं लेता, सामाजिक विकास में भी वह पिछड़ जाता है।
समायोजन की समस्याओं के अतिरिक्त ऐसे बच्चों को संवेगात्मक समस्याओं और शारीरिक तथा मानसिक विकास की समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे बालक संवेगात्मक रूप से परिवर्तित नहीं हो सकते। इनका मानसिक विकास भी सामान्य बालकों की तरह नहीं हो पाता।
शिक्षकों एवं माता-पिता की भूमिका -उपर्युक्त समस्याओं की ओर अध्यापक और माता-पिता को ध्यान देना अनिवार्य है ताकि ऐसे अपंग बालकों का घर, स्कूल तथा समाज में उचित रूप से समायोजन हो सके और वे किसी पर बोझ न बनकर अपने पैरों पर खड़े हो सकें।
विकलांग बालकों की शिक्षा
शारीरिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ संभव नहीं है। इन विकलांग बालकों को अधिगम और समायोजन सम्बन्धी विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन समस्याओं के परिणामस्वरूप बालकों में हीन भावना का विकास होता है।
अतः विभिन्न दृष्टिकोणों से विकलांग बालकों के लिए विशेष शैक्षिक सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है।
1. अपंग बालकों की शिक्षा - अपंग बालकों में शारीरिक दोष होने के कारण वह अपने शरीर के विभिन्न अंगों का समायोजन नहीं कर सकता और यही उसका सबसे बड़ा अवरोधक होता है। अतः ऐसे बालकों के लिए शिक्षा में विशेष व्यवस्था की जानी चाहिए।
(1) मानसिक स्तर - अपंग बालकों का मानसिक स्तर सामान्य जैसा होता है। अतः उन्हें उनके साथ ही शिक्षा ग्रहण और मानसिक विकास के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए।
(2) उनके शारीरिक दोष के अनुसार ही उनके बैठने के लिए कुर्सी-मेज की व्यवस्था होनी चाहिए।
(3) उन्हें विशेष व्यवसायों का प्रशिक्षण भी मिलना चाहिए ताकि वे दूसरों पर बोझ न बन सकें। उनके शारीरिक दोष का ध्यान रखा जाना चाहिए।
(4) विकलांग बच्चों को विकल अंगों के डॉक्टरों के पास भेजना चाहिए ताकि विकल अंगों के ऑपरेशन द्वारा ठीक होने के अवसरों का लाभ उठाया जा सके। इसके लिए कृत्रिम अंगों की व्यवस्था होनी चाहिए। इस कार्य के लिए विकलांग बालकों के माता-पिता को शिक्षित करना अति आवश्यक है।
(5) विकलांग बच्चों को अपनी रुचि के बारे में दृष्टिकोण बदलने की शिक्षा देनी चाहिए और दूसरे सामान्य लोगों के साथ संपर्क बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।
(6) निशक्त या विकलांग बालकों का सामाजिक समायोजन करना बहुत आवश्यक है। इनके मन में हीन-भावना को दूर करना शिक्षा का केंद्र बिंदु होना चाहिए।
2. संपूर्ण और अर्ध-अंधों की शिक्षा- संपूर्ण रूप से अंधे या आधे-अंधे बालकों की शिक्षा के लिए अध्यापक को निम्न प्रयास करने चाहिए-
(1) इनका उपचार किसी विशेषज्ञ से ठीक हो सके तो इनके लिए ऐसों का प्रबंध करना चाहिए।
(2) बिल्कुल अंधे बालक सामान्य शिक्षण पद्धति के अनुसार नहीं चल सकते और न ही सामान्य बालकों के साथ वे उसी प्रकार सीख सकते हैं। अतः इन्हें अन्य-विद्यार्थियों से भेज देना चाहिए जहाँ पर ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए विशेष विधियाँ प्रयोग की जाती हैं।
(3) इनके लिए मोटे टाइप की पुस्तकों का प्रयोग होना चाहिए।
(4) ऐसे बालकों की कक्षाओं में हवा और रोशनी का उचित प्रवाह होना चाहिए।
(5) इन बालकों की लिखाई-पढ़ाई की आदतों में सुधार किया जाना चाहिए।
(6) श्यामपट्ट स्पष्ट लिखने वाला हो ताकि इसपर लिखी हुई सामग्री को ये बालक उचित प्रकार से पढ़ सकें। साथ ही, श्यामपट्टों का स्थान इतनी दूरी पर हो कि बालकों की आँखों पर किसी प्रकार का दबाव न पड़े।
(7) पूर्ण या अपूर्ण अंधे बालकों को पुस्तकीय ज्ञान की अपेक्षा किसी हस्त-कला का प्रशिक्षण मिलना चाहिए।
3. पूर्ण बहरे या अपूर्ण बहरे की शिक्षा- बिल्कुल बहरे बच्चे वे होते हैं जिन्हें बिल्कुल भी सुनाई नहीं देता। ये या तो जन्म से बहरे होते हैं या किसी रोग के कारण बहरे हो जाते हैं। कई बच्चे सुनते तो हैं लेकिन कम सुनते हैं। ऐसे बालकों को सामान्य बालकों की तरह नहीं सिखाया जा सकता। इनकी शिक्षा की निम्नलिखित व्यवस्थाएँ होनी चाहिए-
(1) बहरे बालकों के लिए विशेष प्रकार के स्कूलों की व्यवस्था की जानी चाहिए। इन स्कूलों में इनका प्रशिक्षण दिया जाता है। कई शहरों में ऐसे स्कूलों की व्यवस्था है- गुजरात, रोहतक, दिल्ली आदि। ऐसे बालकों के माता-पिता को शिक्षण की प्रक्रिया का ज्ञान दिया जाना चाहिए। ऐसे स्कूल अमेरिका के लॉस एंजेल्स में जॉन ट्रेसी की निदानशाला है जो इनका विशेष प्रशिक्षण देती है।
(2) कम बहरे बच्चों के लिए अलग स्कूलों की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए क्योंकि ऐसे बालक अध्यापक के होठों से बहुत-कुछ जान सकते हैं व सीख सकते हैं।
(3) ऐसे बालकों और अध्यापकों में अच्छे सम्बन्ध स्थापित होने चाहिए ताकि उनके समायोजन के लिए अध्यापक व्यक्तित्व ध्यान दे सकें।
4. हकलाने वाले या दोषपूर्ण वाणी वाले बालकों की शिक्षा- दोषपूर्ण वाणी में हकलाना, तुतलाना, बहुत धीरे बोलना या बहुत मोटी आवाज में बोलना या बिल्कुल ही न बोलना इत्यादि दोष शामिल होते हैं। अस्पष्ट बोलना भी वाणी दोष में सम्मिलित है। इन दोषों के कारण बालकों में हीन-भावना, आत्म-विश्वास की कमी, संवेगात्मक अस्थिरता आदि का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। अतः ऐसे बालकों के विशेष शिक्षा का प्रबंध होना अति आवश्यक है। इसके लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं-
(1) इनके साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार होना चाहिए।
(2) अध्ययन की गलत आदतों पर नियंत्रण करना आना चाहिए।
(3) योग्य डॉक्टरों का परामर्श लेना तथा इलाज कराना चाहिए।
(4) विशेष शब्दों का उच्चारण बार-बार कराया जाना चाहिए।
(5) कई बार बिल्कुल न बोलने वाले बालकों को या तो बिल्कुल ही सुनाई नहीं देता या फिर वे ठीक से सुनते हैं। बोलने और सुनने में गहरा सम्बन्ध होता है। अतः ऐसे बालकों को श्रवण-समर्थी द्वारा सुनने के योग्य बनाकर उनकी वाणी में सुधार किया जा सकता है।
(6) बालकों को बोलने का उचित प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
5. निर्बल बालकों की शिक्षा- ऐसे बालकों को कोई रोग तो इनमें कोई शारीरिक दोष तो नहीं होता परन्तु इनका स्वास्थ्य इतना सुदृढ़ नहीं होता। स्वास्थ्य का इन्हें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। इस निर्बलता का कारण दोषपूर्ण पालन-पोषण, असंयमित भोजन या खून के रोगों का आभास होना है। ऐसे बालकों की शिक्षा के लिए डॉक्टरी परीक्षण और मनोवैज्ञानिक की शिक्षण-बीमारियों की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे बालकों को संतुलित भोजन व स्वच्छ पालन-पोषण आवश्यक है।
6. मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की शिक्षा- मानसिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा के लिए निम्नलिखित सुझाव हैं-
(1) अध्यापक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
(2) मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के माता-पिता को शिक्षित करना आवश्यक है।
(3) ऐसे बालकों के लिए विशेष स्कूल या अस्पताल होने चाहिए।
(4) इन बालकों के शिक्षण के लिए विशेष शिक्षण-विद्याएँ अपनाई जानी चाहिए क्योंकि सामान्य शिक्षण-विद्याएँ इन बालकों के लिए अहितकर हैं।
(5) मंद बुद्धि बालकों या मानसिक रूप से विकलांग बालकों का पाठ्यक्रम भी विशेष प्रकार का होना चाहिए। इनको किसी हस्तकला का प्रशिक्षण दिया जाना इनके लिए लाभकारी हो सकता है।
7. संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा- संवेगात्मक और सामाजिक रूप से विकलांग बालकों की शिक्षा और उपचार के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं-
(1) इन बालकों के परिवार के वातावरण में सुधार करना चाहिए।
(2) स्कूल के वातावरण में सुधार करना आवश्यक है।
(3) सामाजिक वातावरण में सुधार करना आवश्यक है।
(4) इन बालकों के उपचार के लिए मनोवैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाये।
(5) इनका उपचार मानसिक चिकित्सा द्वारा होना चाहिए ताकि इनका मानसिक तनाव और द्वन्द्व दूर हो सके।
(6) इनके लिए विशेष बाल-न्यायालय होने चाहिए जहाँ पर कपटाचारियों के बाल-अपराधियों के मामले न किए जाएँ।
कार्यवाही के लिए सुधार-विद्यालयों का होना भी अति लाभकारी सिद्ध हो सकता है। उपर्युक्त विषयों द्वारा विभिन्न प्रकार के विकलांग बालकों की शिक्षा और उनके उपचार का प्रबंध कर सकते हैं। अध्यापक अपना योगदान दे सकते हैं।
|
|||||

 i
i