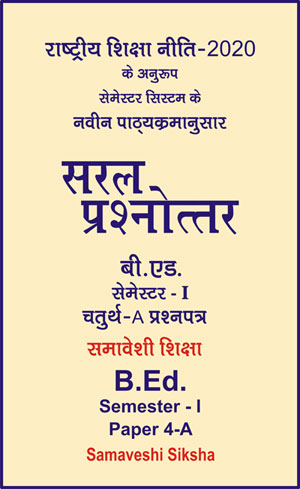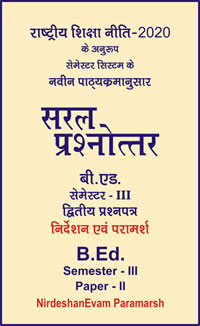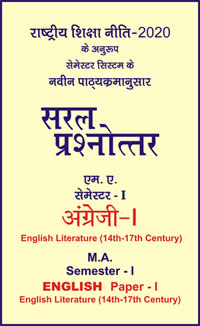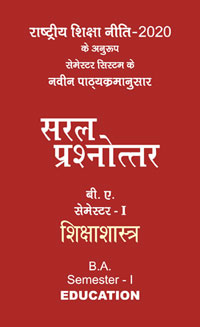|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-A - समावेशी शिक्षा
प्रश्न- दृष्टि बाधिता या दृष्टि असमर्थता का क्या अर्थ है। दृष्टि बाधिता की मुख्य विशेषताओं, पहचान तथा इनकी देखभाल एवं प्रशिक्षण की विवेचना कीजिए।
उत्तर -
दृष्टि बाधिता या दृष्टि असमर्थता का वर्णन करने के दो तरीके हैं -
(a) वैज्ञानिक या कानूनी या मेडिकल परिभाषा- इस परिभाषा में दृष्टि के क्षेत्र का अनुमान लगाया जाता है। इससे यह निर्धारित किया जाता है कि क्या कोई व्यक्ति वैज्ञानिक या कानूनी रूप से अंधा है या नहीं? सन 1934 में अमेरिका मेडिकल एसोसिएशन ने यह परिभाषा स्वीकार की है। कानूनी परिभाषा के अंतर्गत यह देखा जाता है कि व्यक्ति की आँख कितनी दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकती है। इसे हम Snellen chart द्वारा देखा…
जाता है। यदि कोई व्यक्ति एक मीटर की दूरी पर अंगुलियों को नहीं गिन सकता तो वह अंधा माना जाता है। कुछ व्यक्ति आंशिक रूप से तथा कुछ पूर्ण रूप से दृष्टि असमर्थ होते हैं। कुछ लोग आंशिक दृष्टि असमर्थता को निम्न दृष्टि का नाम देते हैं, जोकि उचित नहीं है।
(b) शैक्षिक या कार्यात्मक परिभाषा- कई अध्यापक कानूनी या मेडिकल परिभाषा में विश्वास नहीं रखते हैं तो ऐसा विचार व्यक्त किया जाता है कि कानूनी रूप से अंधे व्यक्ति की दृष्टि नहीं होती जबकि अन्य आँखों का बहुत प्रतिरोध है। पूर्ण अंधता होती है। इनमें से अधिकतर लोग देखने योग्य होते हैं। कानूनी परिभाषा की परिस्तिथि को देखते हुए अधिकतर लोग शैक्षिक परिभाषा को महत्वपूर्ण करते हैं। शैक्षिक उद्देश्य के अंतर्गत वे लोग जो बुरी तरह से दृष्टि बाधित होते हैं और जिन्हें बड़ी छपाई पढ़ने की आवश्यकता होती है, वे दृष्टि असमर्थ कहलाते हैं जो आंशिक रूप से अंधे होते हैं वे मुद्रित शब्दों को पढ़ पाते हैं तथा अक्षरों को पढ़ सकते हैं।
दृष्टि बाधिता/असमर्थता की विशेषताएँ
दृष्टि बाधिता/असमर्थता की मुख्य विशेषताओं का अध्ययन हम निम्न श्रेणियों के अंतर्गत करते हैं-
- भाषा विकास
- बौद्धिक योग्यता
- शैक्षिक उपलब्धि
- सामाजिक और कार्य समायोजन
1. भाषा विकास - (i) दृष्टि बाधिता या असमर्थता की भाषा का विकास बाधित नहीं होता, ऐसी बात अध्ययन के परिणामस्वरूप सामने आई है। अन्य व्यक्ति भाषा से सुन सकता है तथा वह दृष्टिहीन बच्चा को अधिक भाषा का प्रयोग कर सकता है क्योंकि उसके पास स्पर्श का यही मुख्य साधन होता है।
(ii) बहरे ऐसे बच्चों की भाषा बाधित नहीं होती लेकिन यह सामान्य बच्चों की भाषा से भिन्न होती है। सामान्य बच्चों की भाषा उनके संवेदनों व अनुभूतियों के अनुसार ही स्पष्ट होती है परंतु अन्य व्यक्ति "शाब्दिक अव्यावहारिकता" का प्रदर्शन करता है। अर्थात वह शब्दों का अपरिपक्व निम्नतत्त्व का प्रदर्शन करता है।
2. बौद्धिक योग्यता - (i) दृष्टि बाधित बच्चे निम्न बुद्धि वाले नहीं होते। जिन बच्चों का I.Q. शुरू के वर्षों में कम होता है वे अचानक नाटकीय ढंग से पर्याप्त शैक्षिक सुविधाओं के कारण बुद्धि का प्रदर्शन करते हैं।
(ii) अच्छे बच्चों की संप्रेषणात्मक योग्यताएँ सामान्य बच्चों से निम्न स्तर की नहीं तो अलग अवश्य होती हैं। संप्रेषणात्मक विकास में कमी पर्याप्त अनुभवी अनुभवों के अभाव के कारण होती है।
(iii) ऐसे बच्चे स्थान को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं व दूरी को नहीं देख सकते। वे स्थान का अनुमान किसी स्थान पर पहुँचने में लगे समय के आधार पर करते हैं, आवाजों से वे निकट और दूरी का अनुमान प्राप्त करते हैं।
(iv) ऐसे बच्चों में ध्यान की योग्यता अधिक होती है क्योंकि इनका अन्य इंद्रियों पर निर्भरता अधिक होती है। वे कार्य को अच्छी तरह से सुन सकते हैं।
3. शैक्षिक उपलब्धि - (i) आंशिक रूप से और पूर्ण रूप से दृष्टि बाधित बच्चे दृष्टि वाले बच्चों से मानसिक आयु में दृष्टि से पीछे होते हैं।
(ii) दृष्टि बाधित बच्चों की उपलब्धि उतनी प्रभावित नहीं होती जितनी कि श्रवण-बाधित बच्चों की होती है क्योंकि सुनने की योग्यता स्कूल अधिगम के लिए अधिक महत्वपूर्ण है।
4. सामाजिक और कार्य समायोजन - (i) ऐसे बच्चों में यदि समायोजन की समस्या पैदा होती है तो यह इस कारण हो सकती है कि समाज ने उनके साथ अलग प्रकार का व्यवहार किया। दूसरे शब्दों में अन्य व्यक्ति के प्रति समाज की प्रतिक्रिया उसके समायोजन को निर्धारित करती है।
(ii) दृष्टि बाधित बच्चों को उनके साथियों द्वारा उचित प्रकार से स्वीकार नहीं किया जाता है। आंशिक दृष्टि बाधित बच्चों को बाधित बच्चों की अपेक्षा अधिक स्वीकार किया जाता है। हालांकि उनके प्रति समाज सहानुभूति भी बढ़ जाती है।
(iii) यह आवश्यक नहीं होता कि अन्य व्यक्ति अधिक आकर्षण और निराश्रय होते हैं। अंधे बच्चों की निराशा और मिष्क्रियता अंधों के प्रति समाज के दृष्टिकोण और अपेक्षाओं के प्रति परिणाम होती है।
दृष्टि असमर्थियों की पहचान
जो बच्चे जन्म से अंधे होते हैं, उनकी पहचान उनके माता-पिता जल्दी कर लेते हैं लेकिन जिन बच्चों में दृष्टि बाधिता कम होती है, उनकी पहचान प्राथमिक स्कूल से पहले नहीं हो पाती जब स्कूल कार्य में दृष्टि आवश्यक हो जाती है।
इन बच्चों की पहचान के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिक लोगों की सहायता लेनी चाहिए ताकि दृष्टि बाधिता की मात्रा और प्रकृति की पहचान की जा सके। जिन बच्चों की आँखें देखने में सामान्य लगती हैं, उनकी पहचान जल्दी से नहीं हो पाती। अध्ययनकर्ताओं ने बच्चों की पहचान निम्न तरीकों से करने का कार्य किया है, जिसे NCERT, नई दिल्ली ने विकसित किया है। यह ध्यान रहे कि केवल एक ही व्यवहार से इनकी पहचान नहीं होती है, एक से अधिक व्यवहारों का होना आवश्यक है।
1. व्यवहार इसके अनुरूप :
(i) बच्चा आँखों को अधिक मलता रहता है।
(ii) एक आँख को ढक कर सिर आगे को झुकाता है।
(iii) पलकें बहुत बार झपकता है।
(iv) दूर की दृष्टि वाले खेलों में भाग लेने के योग्य नहीं होता।
(v) रोशनी के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होता।
(vi) पुस्तक को आँखों के निकट रखकर पढ़ता।
(vii) कक्षा में बोर्ड से नोट उतारते समय अन्य बच्चों से पूछता।
2. Appearance (दिखावट):
(i) ऐसे बच्चों की आँखें crossed होती हैं।
(ii) पलकें सूजी हुई होती हैं।
(iii) आँखों में पानी भरा होता है।
3. Complaints (शिकायतें):
(i) आँखों में जलन या खुजली का महसूस होना।
(ii) ठीक प्रकार से देख न पाना।
(iii) सिरदर्द रहना, आँखें जोर डालकर काम करने के बाद थकावट का होना।
(iv) धुँधली या दोहरी दृष्टि का होना।
अध्यापक द्वारा ऐसे विद्यार्थियों की पहचान करने के बाद उन्हें विशेषज्ञों के पास भेजना आवश्यक होता है ताकि उनकी मेडिकल जाँच की जा सके। जैसे विद्यार्थियों को उपयुक्त स्कूलो में समायोजित किया जाना चाहिए ताकि वे ठीक प्रकार की शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें।
इनके लिए निम्नलिखित प्रकार के स्कूल हो सकते हैं-
(a) आवासीय स्कूल
(b) नियमित स्कूलों में विशेष कक्षा में इन्हें रखना
(c) एकीकृत ढाँचे में नियमित कक्षा कक्ष में इन्हें स्थापित करना
(d) कई स्कूलों का एक ही इंचार्ज अध्यापक का होना
(a) आवासीय स्कूल -अंधे/अधिक दृष्टि असमर्थ बच्चों को आमतौर पर आवासीय स्कूलों में रखा जाता है। यहाँ अपने माता-पिता से तथा अन्य साथियों से अलग रहते हैं। यह स्थिति सही प्रतीत होती है, लेकिन इस प्रकार का व्यवहार बहुत कम लोकप्रिय है। विशेषज्ञ यह मानते हैं कि आवासीय सुविधा अत्यधिक कम्फर्ट है। अभी हाल ही में यही प्रवृत्ति रही है कि अंधे बच्चों को आवासीय संस्थाओं में न रखा जाए जब तक कि उनमें कोई अन्य न्यूनता न हो, जैसे मानसिक विकलांगता, बहरापन आदि।
बेल सिखाकर इन्हें नियमित कक्षा में रखना चाहिए। ऐसी सरकार की योजना है असमर्थ बच्चों के लिए एकीकृत शिक्षा का नाम दिया गया है।
(b) विशेष कक्षा में रखना - इन्हें विशेष कक्षा में रखना लोकप्रिय विधि है। बच्चा अपना सारा समय विशेष कक्षा में बिताता है तथा नियमित स्कूल में ही रहता है। विशेष रूप में प्रशिक्षित और शिक्षित अध्यापक उनके शिक्षण का कार्य करेंगे।
(c) संसाधन कक्षा की सुविधा वाली कक्षा में रखना - यह विधि सब से अधिक प्रभावशाली है। इस व्यवस्था के अंतर्गत बच्चे दृष्टि वाले बच्चों के साथ रहते हैं। वे उनके साथ नियमित कक्षा में आधा दिन व्यतीत करते हैं और नियमित अध्यापक द्वारा पढ़ाया जाता है। विशेष अनुशरण के लिए उन्हें संसाधन कक्ष में ले जाया जाता है, ताकि संसाधन अध्यापक की सहायता से वे सीख सकें। बच्चों एवं शिक्षण अध्यापक और संसाधन अध्यापक की सहभागिता उत्त्साहित होता है। यह व्यवस्था तभी प्रभावशाली होगी जब अंधों की संख्या नियमित स्कूलों में पर्याप्त होगी।
(d) कई स्कूलों का एक ही इंचार्ज अध्यापक - जब अंधों की संख्या अधिक नहीं होती तथा एक ही स्कूल में एक संसाधन अध्यापक की नियुक्ति संभव न हो, ऐसी स्थिति में एक ही संसाधन अध्यापक कई स्कूलों का इंचार्ज बना दिया जाता है तथा वह हर स्कूल में घूम-घूमकर अंधे बच्चों को विशेष निर्देश प्रदान करता है। यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय है।
दृष्टि असमर्थ बच्चों की देखभाल और प्रशिक्षण
हर बच्चे को चाहें वे किसी भी प्रकार से असमर्थ क्यों न हो, या सामान्य ही क्यों न हो, उपयुक्त शिक्षा एवं प्रशिक्षण प्राप्त करने का अधिकार है। हर समाज को यह अधिकार दृष्टि असमर्थ बालकों को भी प्रदान करना चाहिए ताकि वे भी समाज के लाभकारी सदस्य बन सकें। दृष्टि असमर्थ बच्चों में कई प्रकार के बच्चे शामिल हो सकते हैं- जैसे पूर्ण अंधे, आंशिक दृष्टि असमर्थ, कम दृष्टि वाले तथा एक आँख वाले। शिक्षा और प्रशिक्षण तथा देखभाल दृष्टि दोष के अनुसार ही होनी चाहिए।
ऐसी देखभाल, शिक्षा और प्रशिक्षण माता-पिता, अध्यापक और समुदाय के सदस्यों की सहभागिता से संपन्न हो सकती है। नीचे दी गई विधियों का प्रयोग किया जा सकता है -
1. मोटी टाइप वाली मुद्रित सामग्री - आंशिक रूप से असमर्थ बच्चों को मोटी टाइप वाली मुद्रित सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए। ऐसी पुस्तकों में टाइप मोटा होता है। इनके लिए 18 पाइंट टाइप की सिफारिश भी की जाती है। इससे पढ़ने की गति कम हो जाती है।
2. ब्रेल - जो बच्चे नियमित प्रिंट सामग्री का प्रयोग करने में असमर्थ होते हैं, उन्हें ब्रेल में प्रशिक्षण प्रदान करना चाहिए। यह अंधों के पढ़ने और लिखने की एक मूल प्रणाली है। यह 6 डॉट सेल की बनी होती है जो 63 भिन्न-भिन्न चरित्रों को बताती है। 26 Dots का प्रयोग 26 अक्षरों के लिए किया जाता है तथा बाकी 33 Dots विभिन्न अंक व प्रतिकों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हालांकि, ब्रेल पुस्तकों को संजोकर रखना कठिन होता है क्योंकि ये बहुत मोटी व महंगी होती हैं और संग्रहण के लिए अधिक स्थान लेती हैं। यह कई विषयों और भाषाओं में उपलब्ध नहीं होती।
3. बोलने वाला कैल्कुलेटर - आंशिक रूप से दृष्टि असमर्थ बच्चों को बोलने वाले कैल्कुलेटर का प्रयोग किया जा सकता है। इससे संख्यात्मक प्रक्रियाओं को ईयरफोन द्वारा सुना जा सकता है। गणित को सीखने के लिए अंधे बच्चे इससे अधिक लाभ उठा सकते हैं।
4. टेपरिकॉर्डर - उच्च स्तर की पाठ्य-पुस्तकों या पाठ्य-सामग्री को अध्यापक "टेप" करके अंधे बच्चों को सुना सकते हैं। टेप रिकॉडर का प्रयोग आधुनिक अधिक लोकप्रिय हो रहा है। विशिष्टतः भाषा, इतिहास, भूगोल, विज्ञान आदि के शिक्षण में इस प्रकार का माध्यम से अधिक जानकारी और शिक्षा दी जा सकती है। दृष्टि वाले बालक अनुभव से अधिक ज्ञान अर्जित करने में आगे होते हैं जबकि दृष्टि बाधित बालक "टच" से सूचना ग्रहण करते हैं।
5. मैग्निफाइंग शीशा- आंशिक रूप से दृष्टि वाले बच्चे इस प्रकार के शीशे का प्रयोग कर सकते हैं ताकि वे मुद्रित सामग्री को बड़े स्वरूप में पढ़ सकें।
6. क्लोज़ सर्किट टेलीविजन - आंशिक रूप से दृष्टि असमर्थ बच्चों के लिए क्लोज़ सर्किट टेलीविजन का प्रयोग पश्चिमी देशों में किया जा रहा है। कैमरे द्वारा पुस्तक के पृष्ठ को स्कैन कर उसे टेलीविजन की स्क्रीन पर बड़ा करके दिखाया जाता है।
7. समान पाठ्यक्रम - बहुत से विशेषज्ञ यह मानते हैं कि अन्य बच्चों को सामान्य विधियों द्वारा ही शिक्षित किया जाना चाहिए तथा उन्हें सामान्य सिद्धांतों का पालन करते हुए दृष्टि वाले बच्चों के साथ ही शिक्षित किया जाए। यह कार्य नियमित स्कूलों में ही हो और एकीकृत स्थिति में हो। अध्यापक को चाहिए कि-
(i) जहां तक व्यवहारिक हो, दोहरे अनुभव प्रदान किए जाएं।
(ii) अनुभवों में संशोधन किया जाना चाहिए तथा सामग्री को प्रकारों में, विधियों में भी परिवर्तन किया जाना चाहिए।
(iii) जो पाठ दृष्टि वाले बच्चे को दिया जाता है, उसी से मिलता-जुलता पाठ ही दृष्टि-असमर्थ बालकों को भी दिया जाना चाहिए।
8. सहगामी क्रियाएं - स्कूल में दृष्टि-असमर्थ बच्चों को सहगामी क्रियाओं में भाग लेने के अवसर प्रदान करने चाहिए। उनकी दृष्टि बाधित को ध्यान में रखकर ये क्रियाएं उनसे कराई जा सकती हैं। गाना गाना, यंत्र वादन, भाषण, कविता की रचना करना, खेल जिसमें आवाज का साथ हो जैसे साधारण गेंद के साथ घंटे बजने की व्यवस्था हो। इन गतिविधियों में दृष्टि बाधितों को दृष्टि वाले बच्चों के बराबर रखना ठीक नहीं होगा।
अध्यापक की भूमिका - दृष्टि-असमर्थ बच्चों के समायोजन में अध्यापक की मुख्य भूमिका निम्न प्रकार की हो सकती है -
(i) नियमित अध्यापक ऐसे बच्चों में स्वतंत्रता की भावना पैदा करने के उद्देश्य से उन्हें कम से कम अपनी चीजों की स्वयं देखभाल करने के लिए कहें।
(ii) नियमित अध्यापक दृष्टि-बाधित और सामान्य दृष्टि वाले बच्चों में स्वस्थ अन्तरक्रिया को प्रोत्साहित करें।
(iii) नियमित अध्यापक दृष्टि-बाधित और सामान्य दृष्टि वाले बच्चों को एक समान विशेष कक्षा प्रदान करें।
(iv) अध्यापक कक्षा में सामान्य दृष्टि वाले बालक को दृष्टि असमर्थ बच्चों को ‘गाइड’ बनने को भी कह सकता है।
(v) अंधे बच्चों के साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए, जैसा कि उसके अन्य सामान्य साथियों के साथ किया जाता है।
(vi) दृष्टि असमर्थ बच्चों की शिक्षा की योजना बनाते समय नियमित अध्यापक को संसाधन अध्यापक से विचार-विमर्श अवश्य कर लेना चाहिए। वह नियमित अध्यापक का मानसिक भार कम सकता है।
(vii) आंशिक रूप से अंधे बच्चों के लिए नियमित अध्यापक कक्षा में उपयुक्त भौतिक वातावरण सुनिश्चित कर सकता है। जैसे पर्याप्त रोशनी, बैठने की व्यवस्था आदि।
(viii) अध्यापक को चाहिए कि वह कक्षा में श्रवणिक रूप से देखें, न कि अश्रवणिक संकेतों का प्रयोग करें।
(ix) प्रारंभ में अध्यापक को चाहिए कि वह दृष्टि असमर्थ बच्चों को सभी वस्तुओं की दिशा, स्थिति और दूरी, कक्षाओं की स्थिति आदि को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दें।
|
|||||

 i
i