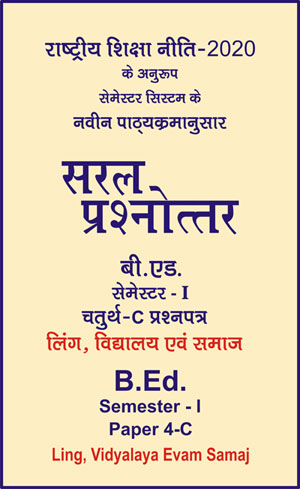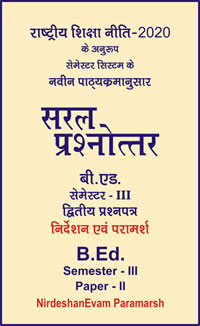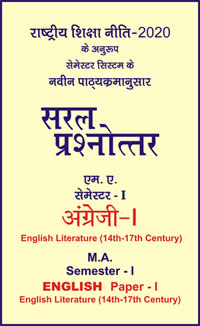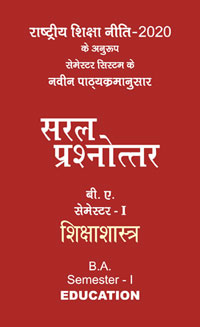|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाजसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज
प्रश्न- जातिगत असमानता क्या है?
लघु उत्तरीय प्रश्न
- जाति पर आधारित विभाजन हमें किस प्रकार प्रभावित कर रहा है?
- जातिवाद किस मान्यता पर आधारित है?
उत्तर-
लिंग और धर्म पर आधारित विभाजन तो दुनिया भर में हैं पर जाति पर आधारित विभाजन सिर्फ भारतीय समाज में ही देखने को मिलता है। सभी समाजों में कुछ सामाजिक असमानताएँ और एक न एक तरह का श्रम का विभाजन मौजूद होता है। अधिकारिक समाजों में पेशा परिवार की एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है। लेकिन जाति व्यवस्था इसका एक अतिवादी अर्थ रखती है। स्थायी रूप से अन्य समाजों में मौजूद असमानताओं से यह एक खास अर्थ में भिन्न है। इसमें पेशे के बंधनात्मक विभाजन को तात्त्विक मान्यता प्राप्त है। एक जाति समूह के लोग एक निश्चित जुलते पेशों से होते हैं। हो सकता है उन्हें दूसरे जाति समूहों के लोगों का काम न देखने दिया जाए। जाति समूह में बेटा-बेटी उन्हीं जाति समूह के लोगों के साथ विवाह करते हैं। अन्य जाति समूहों से उनके बच्चों की न तो शादी हो सकती है न ही महत्वपूर्ण पारिवारिक और सामाजिक आयोजनों में उनकी पंगत में बैठकर दूसरी जाति के लोग भोजन कर सकते हैं।
वर्ण-व्यवस्था अन्य जाति-समूहों से भेदभाव और उन्हें अपने से अलग मानने की धारणा पर आधारित है। इससे अन्य जातियों के साथ छुआछूत का व्यवहार किया जाता था। यही कारण है कि ज्योतिबा फुले, महात्मा गांधी, डॉ. अंबेडकर और पेरियार रामासामी नायकर जैसे राजनीतिज्ञों और समाज सुधारकों ने जातिगत भेदभाव से मुक्त समाज व्यवस्था बनाने की बात की और उसके लिए काम किया।
इन महापुरुषों के प्रयासों और सामाजिक-आर्थिक बदलावों के चलते आधुनिक भारत में जाति की संरचना और जाति व्यवस्था में भारी बदलाव आया है। आर्थिक विकास, शहरीकरण, साक्षरता और शिक्षा के विकास, पेशा चुनने की आज़ादी और गाँवों में जमींदारी व्यवस्था के कमजोर पड़ने से जाति व्यवस्था के पुराने स्वरूप और वर्ण व्यवस्था पर टिकी मानसिकता में बदलाव आ रहा है। शहरी इलाकों में तो अब ज़्यादातर इस बात का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है कि ट्रेन या बस में आपके साथ कौन बैठा है या रेस्टोरां में आपकी मेज़ पर बैठकर खाना खा रहे आदमी की जाति क्या है?
संविधान ने किसी भी तरह के जातिगत भेदभाव का निषेध किया गया है। संविधान ने जाति व्यवस्था से पैदा हुए अन्याय को समाप्त करने वाली नीतियों का आधार तय किया है। अगर सौ साल पहले कोई व्यक्ति एक बार फिर भारत लौटकर आए तो यहाँ हुए बदलावों को देखकर हैरान रह जाएगा।
बावजूद, रमणीयता में न जाति प्रथा बिलकुल नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के कुछ पुराने पहलू अभी भी बरकरार हैं। और भी ज़्यादातर आर्थिक और सामाजिक स्थिति से जुड़े हैं।
स्पष्ट संवैधानिक प्रावधान के बावजूद छुआछूत की प्रथा अभी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। जाति व्यवस्था के अंतर्गत सदियों से कुछ समूहों को लाभ की स्थिति में तो कुछ समूहों को दबाकर रखा गया है। इसका प्रभाव सदियों बाद आज तक नज़र आता है।
जिन जातियों में पहले से ही पढ़ाई-लिखाई का चलन मौजूद था और जिनके शिक्षा पर पकड़ थी, आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में भी उन्हीं का बोलबाला है। जिन जातियों को पहले शिक्षा से वंचित रखा जाता था उनके सदस्य आज भी स्वाभाविक तौर पर पिछड़े हुए हैं।
यही कारण है कि शहरी क्षेत्रों में भी अनेक जाति के लोगों का अनुपात असमान रूप से काफ़ी ज्यादा है। जाति और आर्थिक हैसियत में काफ़ी निकट का संबंध है।
प्राकृतिकता की तरह जातिवाद भी इस मान्यता पर आधारित है कि जाति ही सामाजिक समुदाय के गठन का एकमात्र आधार है। इस चिंतन पद्धति के अनुसार एक जाति के लोग एक स्वाभाविक समुदाय बनाते हैं और उनका हित सबसे पहले एक जैसे होते हैं तथा दूसरी जाति के लोगों से उनके हितों में टकराव हो ही होता है।
किन्तु मंत्रित्ववाद के मामले में देखा है, यह मान्यता हमारे अनुभव से पुष्ट नहीं होती। हमारे अनुभव बताते हैं कि जाति हमारे जीवन का एक पहलू ज़रूर है लेकिन यही एकमात्र या सबसे महत्वपूर्ण पहलू नहीं है।
|
|||||

 i
i