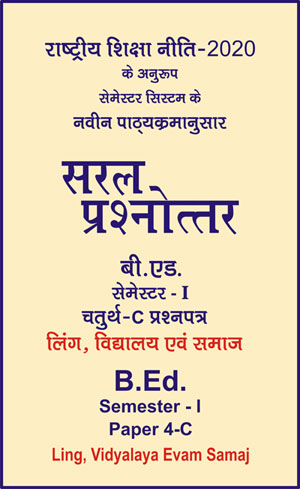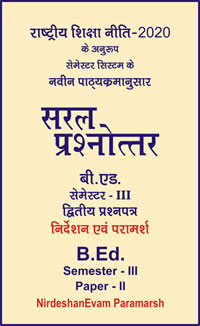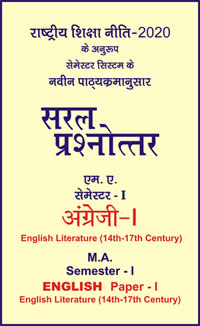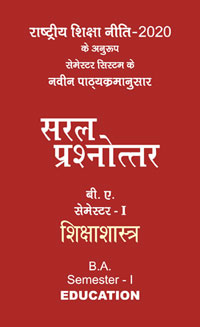|
बी एड - एम एड >> बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाजसरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बी.एड. सेमेस्टर-1 प्रश्नपत्र- IV-C - लिंग, विद्यालय एवं समाज
प्रश्न- टिप्पणी लिखिए— महिलाओं के प्रति होने वाली हिंसा।
लघु उत्तरिय प्रश्न
- भारत में दहेज उत्पीड़न के कितने मामले सामने आते हैं?
- वे कौन-सी वैधानिक धारणाएँ हैं जिनके कारण कोई महिला हिंसा के विरुद्ध अपनी आवाज नहीं उठाती?
उत्तर-
महिलाओं के विरुद्ध हिंसा शारीरिक और मनोवैज्ञानिक दोनों तरीकों की होती है। आक्रमण और हिंसा पुरुषों की सामाजिक रूप से स्वीकृत विशेषताओं में पितृसत्ता में शामिल की जाती है। समाज में लगातार जारी दहेज की प्रथा यह सिखा करती है कि महिलाओं के विरुद्ध हिंसा एक व्यवस्थित मुद्दा है जिसे सुनियोजित तरीके से सम्बोधित करने की आवश्यकता है। यह एक बहुत जटिल परिस्थिति है जिसके अन्तर्गत हिंसा के अनेक आयाम शामिल रहते हैं। भारत में दहेज के लिये प्रतिवर्ष लगभग 22 महिलाएँ जान से मारी दी जाती हैं। पिछले तीन वर्षों में सम्पूर्ण देश में दहेज से जुड़ी लगभग 24,771 मौतें दर्ज की गई हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश में दहेज हत्या की घटनाएँ सर्वाधिक होती हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड्स ब्यूरो के आंकड़ों के मुताबिक देश में लगभग 3.48 लाख मामले ऐसे दर्ज किये गये हैं, जहाँ पतियों या उनके रिश्तेदारों ने महिलाओं पर क्रूरतापूर्ण अत्याचार किया हो। दुःखद मामलों में पश्चिम बंगाल शीर्ष स्थान पर है, जहाँ पिछले तीन वर्षों में इस प्रकार की लगभग 61,259 घटनाएँ दर्ज की गई। इसके बाद 44,311 घटनाओं के साथ राजस्थान दूसरे और 34,835 घटनाओं के साथ मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है (द पायनियर, 2015) 2015 मार्च में प्रकाशित ब्यूनी की रिपोर्ट यह दर्शाती करती है कि लड़कियों और महिलाओं के अपहरण या अवयस्क बहला-फुसलाकर अपने वश में ले जाने के 59,277 मामले (आई.पी.सी. के तहत किये गये कुल आपराधिक मामलों का 2.01 प्रतिशत); छेड़खानी के 82,422 मामले (आई.पी.सी. के तहत किये गये कुल आपराधिक मामलों का 2.79 प्रतिशत) यौन-उत्पीड़न के 24,041 मामले (आई.पी.सी. के तहत किये गये कुल आपराधिक मामलों का लगभग 1.18 प्रतिशत) तथा बलात्कार के 34,771 मामले (आई.पी.सी. के तहत किये गये कुल आपराधिक मामलों का 1.18 प्रतिशत) दर्ज हुए घरेलू हिंसा से महिलाओं की रक्षा के लिये बनाये गये 2005 के कानून (PWDVA) के बावजूद पतियों और उनके रिश्तेदारों द्वारा किये गये क्रूर अत्याचारों के 1,13,403 मामले (आई.पी.सी. के तहत किये गये कुल आपराधिक मामलों का 3.85 प्रतिशत) दर्ज किये गये। इस प्रकार अपराधों की जीवन पर, शिक्षा तक उनकी पहुँच पर और विद्यालयों में उनके द्वारा बेहतर प्रदर्शन किये जाने पर नकारात्मक असर पड़ता है।
किसी भी जगह पर घटित होने वाले अपराध की दर उन प्राथमिक सूचकों मे से एक होती है जो उस जगह पर प्रचलित सामाजिक-आर्थिक स्थिति और वहाँ की न्याय प्रणाली की कुशलता को प्रतिबिम्बित करते हैं। जिन महिवाओं के साथ बलात्कार किया जाता है या जिन पर यौनिक आक्रमण किया जाता है, उनमें से अधिकांश महिलाएँ बहुत सारे मामलों में उन अपराधों की शिकायत पुलिस में दर्ज नहीं कराती क्योकि उन्हे इस बात का बहुत कम भरोसा होता है कि अपराधी को सजा मिलेगी। देश में महिलाओं के विरुद्ध अपराधों को दर्ज न करने के लिये अनेक कारण उत्तरदायी हैं-
महिलाओं से सम्बद्ध अपराधों से जुड़ा सामाजिक लांछन - एक पुरुष-प्रधान वाले समाज में महिलाओं के प्रति किये जाने वाले अपराधों को बहुत महत्व नहीं दिया जाता क्योंकि महिलाएँ इतनी आत्मनिर्भर नहीं होतीं कि वे अपने निर्णय खुद ले सकें और इसलिए वे अपने माता-पिता, सास-ससुर या परिवार के अन्य पुरुष सदस्यों की दया पर निर्भर होती हैं। परिवार में होने वाले अपराधों का दर्ज न कराने के पीछे जो कारण मौजूद हैं, उनमें यह सर्वोपरि कारण है। लज्जा और झिझक तथा अपमान ऊपर से नीचे हलकों को निजी मामलें की तरह रखने को बढ़ावा देने के कारण ही विभिन्न वजह से महिलाएँ अपने खिलाफ होने वाले अपराधों को दर्ज नहीं करा पातीं।
तिरस्कार या अपराधी का डर या अन्य वैयक्तिक धारणाएँ - महिलाओं से सम्बंधित बहुत सारे अपराध इसलिए भी नहीं दर्ज हो पाते क्योंकि अपराधी उन्हें या उनके परिवार को और अधिक नुकसान पहुँचाने की धमकी देते है। अवरोधक तत्व के अभाव को शामिल करते हुए इन कारणों का परिणाम यह होता है कि महिलाओं के विरुद्ध होने वाले सारे अपराध दर्ज नहीं हो पाते।
आपराधिक न्याय प्रणाली में विश्वास का अभाव - न्याय प्रणाली की धीमी गति, जैसा कि भारत में है, भी उन मुख्य कारणों में शामिल है, जिनके कारण महिलाएँ और यहाँ तक कि पढ़ी-लिखी महिलाएँ भी अपने विरुद्ध होने वाले अपराधों को दर्ज कराने में असफल रह जाती हैं।
महिलाओं के विरुद्ध की जाने वाली हिंसा जेंडर दमन की संरचनाओं को बनाए रखती है; चाहे यह निजी क्षेत्र में व्यक्तियों द्वारा हो या फिर सार्वजनिक क्षेत्र में संस्थानिक ताकतों द्वारा पारित हो। जेंडर सामाजिक सम्बन्धों बल के उपयोग का माध्यम से शक्तिशाली प्रयोग भी आंशिक होते हैं। (कनालस और कनालस, 1991)।
शक्ति पिरामिड के लिये डरहरा प्रयुक्त होता है। किन्तु, दुर्व्यवहार या पुरुषत्व के साथ इसे सम्मिलित कर देना समस्यात्मक हो जाता है।
|
|||||

 i
i