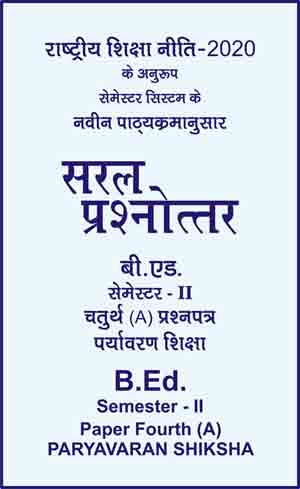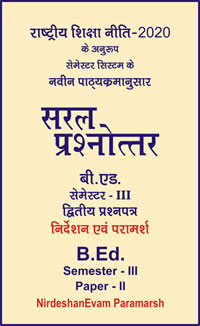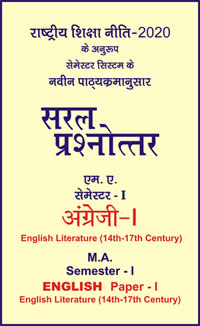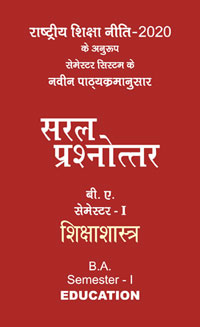|
बी एड - एम एड >> बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षा बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षासरल प्रश्नोत्तर समूह
|
|
||||||
बीएड सेमेस्टर-2 चतुर्थ (A) प्रश्नपत्र - पर्यावरणीय शिक्षा - सरल प्रश्नोत्तर
प्रश्न- निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए- (a) ताजमहल विवाद (b) भोपाल गैस त्रासदी (c) परमाणु दुर्घटना
उत्तर-
(a) ताजमहल विवाद
समस्या - ताजमहल आगरा में स्थित हमारे देश की महत्वपूर्ण सांस्कृतिक धरोहर है । हमेशा से ही यह विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का केन्द्र रहा है। 1972 में सरकार ने मथुरा में एक तेल परिशोधनशाला की स्थापना का निर्णय लिया तो अनेकों पर्यावरण वैज्ञानिक एवं पुरातत्व वेत्ताओं ने इस औद्योगिक संस्थान के कारण भविष्य में होने वाले प्रदूषण से ताजमहल पर हानिकारक प्रभावों की आशंका व्यक्त की। इस तेल परिष्करणशाला में प्रयुक्त किये जाने वाले ईंधन से उत्पन्न धुएँ में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक रहती है। यह सल्फर डाईऑक्साइड वर्षा के जल के साथ वायुमंडल से पृथ्वी पर सल्फ्यूरिक अम्ल के रूप में आती है। इस कारण इस उद्योग की स्थापना से आगरा की वायु में भी सल्फर डाइऑक्साइड तथा वर्षा जल में सल्फ्यूरिक अम्ल के बढ़ने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। चूँकि सल्फ्यूरिक अम्ल संगमरमर जैसे पत्थरों को भी प्रभावित करता है, इसलिए पारिस्थितिक वैज्ञानिकों की ताजमहल के प्रति आशंका निर्मूल भी नहीं कही जा सकती है।
समाधान - सरकार ने इस सम्बन्ध में सही-सही जानकारी प्राप्त करके सन् 1974 में कमेटी की नियुक्ति की । इसी बीच भारतीय तेल निगम ने भी इटली की मेसल्स टेक्निको नामक अभियांत्रिकी फर्म को परिष्टकरण संस्थान की स्थापना से आगरा की वायु में होने वाले गुणोत्तम परिवर्तनों के आकलन का भार सौंपा। इस फर्म तथा शासकीय समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट हो गया है कि मथुरा में स्थापित होने वाली इस तेल परिष्करण संस्थान से आगरा की वायु में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा में बहुत नगण्य वृद्धि होगी। अतः मथुरा तेल परिष्करणशाला की स्थापना का ताजमहल पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस विवाद का कोई तात्कालिक लाभ चाहे भले ही न हुआ हो पर आज यह परिवर्तन निश्चित ही आया है कि बड़े उद्योगों की स्थापना के पूर्व केन्द्र तथा राज्य सरकारें इन उद्योगों के पर्यावरणीय प्रभावों का आकलन कराने के प्रति सतर्क रहती हैं।
(b) भोपाल गैस त्रासदी
दो-तीन दिसम्बर, 1984 की मध्य रात्रि में भोपाल में स्थित यूनियन कार्बाइड, इंडिया (लिमिटेड) के कारखाने के एक संयंत्र में दुर्घटनावश निकली गैसों के कारण अनेक लोगों की जानें गयीं तथा असंख्य लोग विपरीत रूप से प्रभावित हुए। यह घटना 'भोपाल गैस त्रासदी' के नाम से जानी जाती है।
यूनियन कार्बाइड के कारखाने में मिथाइल आइसोसायनेट (एम. आई. सी.) एवं फॉस्जीन का उपयोग सीवान नामक कीटनाशक उत्पाद बनाने में किया जाता था। दुर्घटना का कारण मिथाइल आइसो-सायनेट संयन्त्र की तीन स्टेनलैसस्टील तथा कंक्रीट कवच युक्त भण्डारण टंकियों में से एक में असावधानीवश जल प्रवेश के फलस्वरूप अत्यधिक दाब बढ़ जाना कहा जाता है। दाब की अधिकता से स्टोरेज टंकी की एम. आई. सी. सुरक्षा वाल्व द्वारा बाहर निकलने लगी। अनेक प्रयासों के बावजूद भण्डारण टंकी में जल प्रवेश से शुरू हुई प्रक्रिया तथा फलतः बढ़ रहे दबाव को रोक पाना सम्भव नहीं हुआ। दुर्भाग्यवश गैसों को निष्प्रभावी करने की संयन्त्र की व्यवस्था भी उस रात निष्क्रिय थी। इस कारण संयन्त्र से निकली विषैली गैस आस-पास के वातावरण में तेजी से फैलने लगी। कहा जाता है कि संयन्त्र से निकली गैसों में एम. आई. सी. के एक साथ और बहुत ही विषैली गैस - फॉस्जीन भी थी।
सरकारी आँकड़ों के अनुसार लगभग दो हजार लोगं अकाल को प्राप्त हुए तथा हजारों लोग आँख और श्वास की गम्भीर पीड़ा के शिकार हुए। मनुष्यों के अलावा जानवर तथा पेड़-पौधे भी विपरीत रूप से प्रभावित हुए। इन तात्कालिक प्रभावों के अलावा दूरगामी प्रभावों की शंका भी वैज्ञानिकों द्वारा प्रकट की जा रही है।
उस रात मानो भोपाल ने एक गैस चेम्बर का रूप ले लिया था। लोग कीड़े-मकौड़ों की तरह तड़प-तड़प कर मर रहे थे। स्थिति की गम्भीरता का अन्दाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि विश्व भर में अब तक हुई बड़ी औद्योगिक दुर्घटनाओं तथा वायु प्रदूषण के सबसे खतरनाक उदाहरण के रूप में इस घटना का उल्लेख किया जा रहा है। इस घटना ने जहाँ पर्यावरणीय खतरों के प्रति विश्व जनमत लगाया है, वहीं दूसरी ओर इससे तीसरी दुनिया के गरीब देशों को विकसित राष्ट्रों द्वारा निर्यात की जा रही मुनाफाखोर संस्कृति का असली रूप भी उजागर हुआ। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी मुस्तफा कमान तोल्बा ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है- "गरीब देश अन्तर्राष्ट्रीय कचरा टोकरियाँ बन गये हैं । इस स्थिति को बदलने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ऐसी आचार-संहिता बनाने पर विचार कर रहा है, जिससे अन्तर्राष्ट्रीय कम्पनियाँ तीसरी दुनिया का शोषण न कर सकें। " शायद भोपाल त्रासदी इस दिशा में विश्व जनमत को उभारने में सहायक हो।
(c) परमाणु दुर्घटना
26 अप्रैल, 1986 को प्रातः एक बजकर चौबीस मिनट पर सोवियत संघ के उक्राईन प्रान्त की राजधानी किएफ के समीप स्थित चेरनोबिल परमाणु बिजली घर की चौथी रिएक्टर ड्रा इकाई में ऐसी परमाणु दुर्घटना हुई, जिसने तमाम विश्व को हिलाकर रख दिया। इस यूनिट की चौथी रिएक्टर इकाई की छत पिघल गई और उससे निकली रेडियोधर्मिता वातावरण में फैल गई। इस रेडियोधर्मिता से यूरोप के देश काफी प्रभावित हुए। यही नहीं, इसका प्रभाव टोकियो और वाशिंगटन जैसे दूरस्थ नगरों के वातावरण में भी महसूस किया गया। लेकिन वास्तविकता यह है कि इस प्रकार रेडियोधर्मिता धूल का सामना करने के लिए न तो ये देश तैयार ही थे और न ही इस धूल का कोई साधन आज विश्व के पास उपलब्ध है।
इस दुर्घटना से पहले 1979 में थ्री माइल आइसलैण्ड रिएक्टर के मुख्य भाग से जब रेडियोधर्मिता रिसी थी, तब इसका काफी सारा भाग रिएक्टर के बाहरी आवरण ने ही सोख लिया था, लेकिन चेरनोबिल दुर्घटना में तो 1000 टन स्टील आवरण को भेदकर काफी रेडियोधर्मिता वातावरण में प्रवेश कर गई।
चेरनोबिल रिएक्टर लगभग 10 दिनों तक चलता रहा और इससे रेडियोधर्मिता भी निकलती रही और रेडियोधर्मिता की अच्छी खासी मात्रा इस प्लांट में 2000 किमी. की दूरी तक लगभग 20 देशों में पहुँच गई। रेडियोधर्मिता के डर से दुर्घटना के 36 घण्टे बाद ही लगभग 1000 बसों द्वारा 49,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया। इसके अलावा प्लांट के 10 किमी. के घेरे के निवासियों को भी वहाँ से हटा दिया गया। लेकिन कुछ समय बाद 30 किमी. के घेरे में 49,000 लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया। बाद में स्थिति की गम्भीरता को देखकर कुल मिलाकर 1,35,000 नागरिकों को हटाया गया। किएफ में समय से पहले ग्रीष्म अवकाश करके छात्रों को भी अन्यत्र भेज दिया गया। रेडियोधर्मिता की कितनी मात्रा मनुष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकती है इस बारे में हिरोशिमा व नागासाकी में गिराये गये परमाणु बम के विकिरण के बारे में जानकारी एकत्र की गई है। इस जानकारी से पता चलता है कि अधिक रेडियोधर्मिता के शरीर पर पड़ने से मौत तक हो जाती है। अमरीकी डाक्टर रॉबर्ट मल का कहना है कि चेरनोबिल दुर्घटना के कारण फैली रेडियोधर्मिता के कारण कैंसर द्वारा 5000 से 50,000 तक अतिरिक्त मौतें होंगी। अधिकांश लोगों का मानना है कि चेरनोबिल दुर्घटना से होने वाली हानि इन अनुमानों से कहीं अधिक होगी।
विश्व चेरनोबिल जैसी दुर्घटना के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था और रेडियोधर्मी विकिरण के बचाव का कोई प्रभावशाली साधन तो विश्व के पास आज भी नहीं हैं। बस अपने-अपने स्तर जिससे जो बन पड़ता है करता है।
|
|||||

 i
i